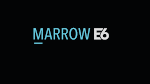Emily Esfahani Smith
व्यर्थ से अर्थ की ओर जीवन का सफ़र
दो लफ्जों में -:
2017 में लिखी इस किताब में लेखिका ने सफल और संतुष्ट जीवन के चार स्तंभों के बारे में बताया है। यूँ तो पृथ्वी पर आयें हैं तो अपना कार्यकाल पूरा कर के एक न एक दिन सबने परमात्मा में लीन हो जाना है लेकिन अंतिम समय आने से पहले जीवन को व्यर्थ से अर्थ की ओर ले जाने का सफ़र इस किताब के जरिये आप तय कर सकते हैं।
ये किताब किसके लिए है?
· साइकोलॉजी, साहित्य या फिलोसोफी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए।
· जो लोग अध्यात्म और परोपकार के मार्ग पर चलकर जीवन का अर्थ ढूंडना चाहते हैं।
· जो जीवन की विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए किसी प्रेरणा की तलाश में हैं।
लेखक के बारे में -:
लेखिका एमिली इस्फ़हानी स्मिथ (Emily Esfahani Smith) सांस्कृतिक और मनोचिकित्सा से जुड़े अपने बेहतरीन लेखों के लिए काफी मशहूर हैं। उनके द्वारा लिखे प्रेरनादायी शब्दों को कई पत्रिकायों नें अपने अंकों में छापकर दुनिया तक पहुँचाया है। लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाने के अपने अथक प्रयासों नें उन्हें स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी (Stanford University)के हुवर इंस्टीट्यूशन (Hoover Institution) का एडिटर बना दिया, इसके बाद से आज तक वो इसी मंच के जरिये लोगों को अपने विचारों से अवगत करवा रहीं है।
यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए
जीवन कि भागदौड़ में अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमें इश्वर नें जीवन जीने के लिए दिया है किसी मशीन की तरह दिन रात काम करने के लिए नहीं। आजकल के बढ़ते प्रतियोगिता के दौर में एकदूसरे को पीछे कर खुद आगे बढाने की दौड़ में इंसान अकेला ही चलता जा रहा है।
अगर कभी इस भागम-भाग से थक कर कोई खुशियाँ तलाश करना भी चाहता है तो भी नहीं कर पता क्यूंकि वो अकेला हीं इतना आगे निकल जाता है कि उसके आस पास उसे कोई नहीं मिलता। इसलिए इस बदलते परिपेक्ष में जीवन का अर्थ कैसे ढूंढे ये सभी बातें आपको इस किताब में मिल जायेंगी। अगर आप जिंदगी को एक नया मौका देना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित होगी।
· खुशियों के चार स्तम्भ कौनसे हैं और उनके बारे में जानना क्यूँ जरुरी है?
· जीवन के कडवे अनुभवों में मिठास का रस कैसे ढूंढे?
· दूसरों के चेहरे पर मुस्कान प्रदान कर कैसे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं?
कुल चार स्तंभों पर टिका है जीवन का अर्थ
जिस तरह एक बहती हुई नदी को रोकना मुश्किल है उसी तरह जीवन भी निरंतर बहता जाता है उसे रोक कर उसका अर्थ ढूंड पाना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक पल का वक़्त जीवन से चुरा कर सोचें की क्या आपके पास जीवन जीने का कोई अर्थ है, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? इन सवालों के उत्तर जानना इसलिए जरुरी है क्यूंकि आज के माहौल में सबकुछ होते हुए भी लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं जिसके कारण पैदा हुई अराजकता लोगों को डिप्रेशन जैसी मानसिक बिमारियों की ओर धकेल देती हैं।
लेखिका का कहना है कि ये बात बिलकुल सच है कि आधुनिकता ने हमें जीवन को सरल बना देने वाली अनगिनत सौगातें दी है, लेकिन एक सच ये भी है कि इस आधुनिक युग में नित नयी तकनीकों के साथ साथ आत्महत्या और मनोरोग जैसी मार्मिक समस्यों की भी बढ़ोत्तरी हुई है।
कई जाने माने मनोचिकित्सकों ने अपनी खोज में इस बात का खुलासा किया है कि पिछड़े और ग्रामीण परिवेशों में रहने वाले लोगों की तुलना में आधुनिकता की गोद में बैठे लोगों में आत्महत्या की घटनाएँ ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो जीवन में खुशहाली लाने के लिए केवल भौतिकतावादी वस्तुयों की नहीं बल्कि एक मकसद की भी जरुरत होती है। ये मकसद हमें जीवन के सच्चे अर्थ का एहसास करवाता है और जीवन में संतोष प्रदान करता है। जीवन का अर्थ चार स्तंभों से मिल कर बना है वो है जीवन का उद्देश्य, जीवन में जुड़े संबंध, हमारे जीवन से जुडी प्रेरणादाई घटनाएँ जिन्हें हम कहानी की तरह किसी को सुना सकें, और जीवन में श्रेष्ठता का अनुभव। इन चारों स्तंभों पर जीवन को व्यर्थ से अर्थ की ओर ले जाने की जिम्मेदारी है। बड़े-बड़े महापुरुषों में से किसी का कहना है कि जीवन का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण सतम्भ है तो कोई कहता है कि जीवन में जुड़े संबंधों का सबसे ज्यादा असर है। चाहे कोई भी युग हो लेकिन कृष्ण से लेकर महात्मा गाँधी तक सबने इन चारों में से हीं किसी न किसी स्तम्भ की बात की है।
आईये आगे के सबकों के जरिये दखते हैं कि कैसे ये स्तम्भ हमें संतुष्ट जीवन की राह दिखाते हैं।
किसी को अपना बनाकर जानें कि ज़िन्दगी के सही मायने क्या हैं।
बढती टेक्नोलॉजी और नित नए सोशल मीडिया एप्लीकेशन नें मानो दुनिया को हमारे कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन में समेट कर रख दिया है। घर बैठे हम दुनिया के किसी भी कोने की खबर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, क्या कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया की सारी खबरें तो हमें होती हैं लेकिन अपने घर और उसमें रहने वालों का हाल हमें नहीं पता होता, अमेरिका में बैठे अपने क्लाइंट से आप रोज़ बात कर लेते हैं लेकिन अपने साथ काम करने वाले दोस्त या आपका घर सजा कर रखने वाली आपकी बीवी के लिए आपके पास वक़्त की हमेशा कमी रहती है।
एक वैज्ञानिक रीसर्च की मानें तो इक्कीसवीं सदी में बच्चों और माँ-बाप के बीच की वार्तालाप का समय मात्र 1 से २ घंटे का रह गया है। सोचिये जिनके साथ आप सारा दिन रहते हैं उनसे हीं आपकी बात नहीं होती। इसलिए लेखिका का कहना है कि अपने आस पास के लोगों से जुड़ना सीख कर हीं हम जीवन के अर्थ को समझ पायेंगे।
जहाँ एक ओर एकल परिवार के बढ़ते चलन के कारण लोग खुद में हीं सिमट कर रह गए हैं वहीँ दूसरी ओर भाग दौड़ भरी ज़िन्दगी नें रिश्तों की डोर को इतना कच्चा कर दिया है कि कब ये डोर टूट कर हमारे हाथों से फिसल जाती है हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए अकेलेपन के शिकार लोग जीवन को व्यर्थ समझने लगते हैं, और समझें भी क्यूँ ना जब सारा दिन चंद पैसों के लिए जद्दोजेहद कर व्यक्ति घर लौटे और उसे उन पैसों का इस्तेमाल करने वाला कोई न मिले तो असंतोष होना तो लाज़मी है।
इसलिए लेखिका नें रिश्तों और संबंधों को जीवन के अर्थ का पहला स्तम्भ माना है क्यूंकि ये रिश्ते हीं हमें जीवन में पूर्णता का एहसास दिलाते हैं। इन रिश्तों को संजो कर रखें ताकी जब भी आप इनकी ओर देखें आपको एहसास हो कि आपका जीवन कितना अर्थ भरा है।
परोपकार और आत्म विश्लेषण से ज़िन्दगी का उद्देश्य ढूंडा जा सकता है।
ज़िन्दगी में उद्देश्य के होने से ज़िन्दगी पूर्ण और सार्थक लगती है ये बात तो सबको पता है, लेकिन उद्देश्य शब्द को सुनते हीं लोगों के मन में कोई बड़ी हीं गहरी और आदर्शवादी बात का ख्याल आता है। असल में जीवन का सही उद्देश्य तो मात्र अपनी क्षमता और संसाधनों को जुटा कर दूसरों की मदद करना है। किसी की मदद करने के लिए आपका करोडपती होकर चैरिटी करना जरुरी नहीं है आप अपने स्तर पर भी किसी की मदद कर सकते हैं बस आपके अन्दर मदद की भावना होनी चाहिए।
उदहारण के तौर पर अगर आप डॉक्टर हैं तो आप गरीब लोगों का मुफ्त इलाज़ कर उनकी मदद कर सकते हैं, अगर आप एक अध्यापक हैं तो आप गरीबों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं इसी तरह आप अपनी कुशलता के अनुसार किसी की मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी जरुरी नहीं है कि एक डॉक्टर या अध्यापक जैसी नौकरी वाले लोग हीं समाज कल्याण का बेडा उठा सकते हैं, आप जो हैं जैसी नौकरी में हैं कुछ न कुछ तो किसी न किसी के लिए आप कर हीं सकते हैं। लेखिका के अनुसार दूसरों की मदद करने का मार्ग ढूंडने के लिए पहले आपको आत्म विश्लेषण करना होगा, एक बार आपने अपनी क्षमतायों को पहचान लिया फिर आप परोपकार की राह पर निकल सकते हैं।
लेखिका नें परोपकार को जीवन का उद्देश्य इसलिए बताया है क्यूंकि जीवन में सबसे ज्यादा संतोष तब होता है जब हमारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, स्वतः हीं उस मुस्कान को देख कर हम अपने सारे गम भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप दूसरों की यूँ हीं मदद करते जायेंगे तो ज़िन्दगी के पन्नों को जब भी पलटेंगे तो आपका जीवन आपको सार्थक हीं लगेगा।
अपने जीवन की कहानियाँ दूसरों से साँझा कर हम उनसे जुड़ सकते हैं और ज़िन्दगी के नए मायनें ढूंड सकते हैं।
वैज्ञानिकों का कहना है कि हर व्यक्ति के अन्दर अपने जीवन से जुडी घटनाओं को किसी कहानी के रूप में प्रस्तुत करने की कला होती है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी कम बोलने वाला क्यूँ न हो अगर उसे मौका मिले तो वो जीवन के अनुभवों को साँझा जरुर करेगा क्यूंकि ये इंसानी दिमाग की खासियत है कि वो दूसरों से अपनी कहानियाँ बाँट कर उनकी राय लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है।
लेकिन हम अपने जीवन को इन कहानियों के जरिये कैसे सार्थक मान सकते हैं? इस सवाल का उत्तर देते हुए लेखिका नें इस सबक में बताया है कि हम किस घटना के बारे में क्या सोचते हैं ये हमारी कहानियों में झलकता है, कोई घटना हमें सकारात्मक प्रभाव वाली लगती है तो उसे हम उत्साह से सुनते हैं और वहीँ किसी नकारात्मक अनुभव को याद कर दुखी हो जाते हैं।
इसलिए अगर जीवन की सार्थकता को समझना है तो जरुरत है कि जीवन की हर कहानी को ऐसे सुनायें की उसमें कोई न कोई सबक छुपा हो जिससे हम ये एहसास कर सकें कि अगर वो घटना हमारे जीवन में न हुई होती तो हमारा जीवन कितना अर्थविहीन होता। जीवन में खुद से ये कभी न पूछें की 'काश ऐसा होता तो क्या होता' बल्कि ये पूछें कि 'अगर ये ना होता तो क्या होता' देखना ज़िन्दगी कितनी सार्थक लगने लगेगी क्यूंकि जो नहीं मिला उसे सोच दुखी होने से अच्छा है जो है उसकी खुशियाँ मनायें।
इस सोच को विज्ञान की भाषा में काउंटरफैक्टूअल थिंकिंग (counterfactual thinking) यानी प्रतितथ्यात्मक सोच का नाम दिया गया है इसमें व्यक्ति तथ्यों के अनुरूप सोचकर किसी घटना का सार निकालता है। इस प्रकार की सोच रख कर हम जीवन के अनुभवों से अधिक से अधिक सीख सकते हैं और ये एहसास कर सकते हैं कि हमें जो मिला वो अच्छे के लिए मिला है, इस प्रकार जीवन का अर्थ ढूंडन भी आसान हो जाएगा।
अपनी श्रेष्ठता समझ कर आप अपने और ब्रह्माण्ड के बीच की दुरी समाप्त कर सकते हैं।
हम दिन भर मेरा-मेरा की रट लगाते रहते हैं पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये मेरा क्या है बस आपका ये हाड-मांस का बना शरीर, इस बात को सोचते हुए खुद से कितनी हीन भावना आने लगती है। लेकिन अगर आप अपनी सोच को थोडा सा बदल कर देखें तो आप समझ पायेंगे कि आप भी इस विशाल ब्रह्माण्ड का हीं एक हिस्सा हैं। कभी रात को टिम-टिमाते हुए तारों को देख कर ये एहसास कीजिये कि आप बस इस शरीर के अन्दर हीं सिमित नहीं हैं बल्कि आप इस विशाल से असमान का एक छोटा सा हिस्सा हैं और ये आसमान आपके अन्दर समाया है और आप इसके, जब भी आप ऐसा सोचेंगे आपको अपने जीवन की श्रेष्ठता का एहसास होगा।
जाने माने मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स (William James) का कहना है कि ये श्रेष्ठता का एहसास इतना सुखद है कि उसे शब्दों में बयाँ कर पाना बहुत हीं मुश्किल है। इस सोच से आप खुद को बड़ा और बेहतर समझने लगते हैं। मै और मेरा के पीछे भागती इस दुनिया में खुद को भूलकर प्रकृति का हिस्सा बन जाना कितना सुकून दायक हो सकता है ये तो आपको खुद हीं अनुभव करना पड़ेगा।
केवल वैज्ञानिक हीं नहीं बल्कि खुद बौद्ध धर्म भी इस भावना की सिफारिश करता है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में इसे ईगो डेथ यानी अहंकार मुत्यु का नाम दिया है। जब इंसान का अहंकार मर जाता है तो उसके पास जीवन को अर्थ देने के बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। स्वयं गौतम बुद्ध का कहना था कि मौत सिर्फ शरीर की होती है आत्मा तो बस एक रूप से दुसरे रूप में बदल जाती है, जिस प्रकार एक बादल कभी नष्ट नहीं होता बल्कि कभी पानी तो कभी भाप बनके इस धरती पर घूमता रहता है।
इंसान जब तक मैं और मेरा करता रहेगा तब तक उसे अपना जीवन अर्थ विहीन हीं लगेगा लेकिन जिस दिन उसनें इस आत्मा की श्रेष्ठता का रहस्य सुलझा लिया उस दिन जीवन की सार्थकता का एहसास उसे खुद-ब-खुद होने लगेगा।
आप किस घटना से क्या सीख लेते हैं ये बात पूर्णतः आपके नज़रिए पर निर्भर करती है।
किसी दार्शनिक नें क्या खूब कहा है कि जो कठिनाई मुझे मार नहीं पाएगी वो मुझे और शक्तिशाली बना देगी। सोचने में ये बात थोड़ी अजीब जरुर लगती है लेकिन ये सच है कि अगर किसी विषम परिस्थिति पर जीत पाने में आप सफल हो जाते हैं तो आपकी क्षमताएं और अधिक बढ़ जाती है।
इस बात को विज्ञान ने भी माना है और कई वैज्ञानिकों नें इस क्षेत्र में कई शोध किये हैं। इन शोधों की मानें तो जो लोग कच्ची उम्र में किसी दुखद घटना का शिकार हुए हैं लेकिन किसी को अपनी पीड़ा न बता पाएं हैं उन्हें आगे जाकर कई मानसिक और शारीरिक बिमारियों का सामना करना पड़ता है, वहीँ दूसरी ओर जो अपनी पीड़ा को किसी के सामने व्यक्त कर पाने में समर्थ रहे वो मानसिक समस्यों से लगभग बचे रहे।
मनोवैज्ञानिक जेम्स पेंनेबेकर (James Pannebacker) ने इस विषय में शोध करने के लिए अपने सभी प्रतिभागियों को कहा कि अपने जीवन के सबसे दुखद और कडवे अनुभवों को एक कागज़ पर लिखें, उन्होंने कहा कि वो ऐसा 15 दिन तक रोज़ करें। कुछ दिनों बाद जेम्स नें ये महसूस किया कि उन सभी लोगों की मानसिक स्थिति में काफी सुधार आया है। ये सुधार इसलिए हुआ क्यूंकि बार-बार उस घटना के बारे में लिख कर एक तो उनका मन हल्का हो गया दूसरा उस घटना के बारे में सोच सोच कर उसका निष्कर्ष निकालना आसान हो गया। एक घटना के हर पहलु को सोचने से व्यक्ति के मन में उस घटना से जुडी सकारात्मक बातें और उससे मिली सीख का आभास होने लगता है इसलिए उनकी पीड़ा खुद-ब-खुद कम होने लगती है।
इसलिए लेखिका का कहना कि जीवन को सार्थक करने के चार स्तंभों को जानने के बाद इस बात का भी ख्याल रखें कि जीवन की हर खट्टी मीठी घटना से कुछ न कुछ सीखें और अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए एक सफल जीवन व्यतीत करें।
जीवन के अर्थ को लेकर समाज की बदलती सोच सुधार का प्रतीक है।
वैसे तो आजकल की युवा पीढ़ी के बीच कमाओ और खाओ की प्रथा बहुत प्रचलित है, पर फिर भी दुनिया के कई कोनों में लोग इस बात का एहसास करने लगे हैं कि बिना अर्थ का जीवन बिना अक्षरों के किताब की तरह है जिसे पढ़ कर कुछ हासिल नहीं हो सकता। सार्थक जीवन के प्रति समाज की बढती रूची के कारण हीं लोग अध्यात्म और परोपकार की ओर खींचे चले जा रहे हैं। आधुनिकता के कारण बढती अराजकता के चलते लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि भौतिकतावादी दुनिया में संतोष प्राप्त करने के लिए विलासिता के साजो सामान की नहीं बल्कि आन्तरिक शांति की जरुरत है।
समाज में कई संस्थानों नें जीवन से नाराज हो चुके लोगों को अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जाने वाली राह पर चलने की प्रेरणा देने की पहल की है। इन संस्थानों का मूल लक्ष्य है कि लोगों के दिलो में सकारात्मकता और परोपकार की भावना उत्पन्न हो ताकि वो जीवन का उद्देश्य समझ सकें और खुद को लोगों से जोड़ते हुए सफल जीवन का निर्वहन करें।
उदहारण स्वरुप हम भारत की जानी मानी एन।जी।ओ। मेक अ विश (Make a wish) को हीं ले लें इस संस्था से जुड़ कर कई लोगों नें जीने की नयी राह को ढूंडा है। ये संस्था लोगों को परोपकार और अध्यात्म का मतलब समझाती है और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने में लोगों की मदद करती है। इस संस्था के जरिये जरूरतमंद बच्चे अपनी इच्छाएं लोगों के सामने रखते हैं और हमारे जैसे कई लोगों को उनकी इच्छाएं पूरी कर उनके चेहरे पर ख़ुशी लाने का मौका मिलता हैं और उनके चेहरे की चमक हमारे जीवन में भी संतोष और सुकून की रौशनी लेकर आती है।
इसलिए लेखिका का कहना है कि अगर आप भी जीवन का अर्थ ढूंडना चाहते हैं तो ऐसी किसी संस्था से जुड़ कर लोगों की सहायता कर अपना जीवन सफल कर सकते हैं।
कुल मिलाकर
जीवन के अर्थ को समझने के लिए सबकुछ छोड़-छाड़ के जंगलों में बस जाना जरुरी नहीं है, आप अपनी रोज़ मर्रा की जिंदगी में मात्र चंद बदलाव कर उसे सार्थक और खुशहाल कर सकते हैं। लेखिका द्वारा इस किताब में बताये सार्थक जीवन के चार स्तंभों को अपने जीवन में उतार कर आप भी अपने जीवन को व्यर्थ से अर्थ की ओर ले जा सकते हैं।
रोज़ मिलने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति से हँसते हुए मिलें
जीवन में हम ना जाने कितने हीं लोगों से मिलते हैं लेकिन उनमें से बस वो हीं लोग हमारी यादों का हिस्सा बनते हैं जिन्होंने कभी ना कभी हमारे दिल को छुया था। तो अगर आप भी लोगों के दिलों को छुना चाहते हैं तो दिन भर में जिस-जिस से भी मिलें मुस्कुरा कर मिलें चाहे वो आपसे पद में छोटा हो या बड़ा किसी को एक मुस्कुराहट का तौफा देने से आपके जीवन में भी खुशियों की लहर आ सकती है।