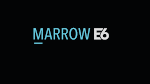John Donvan and Caren Zucker
ऑटिज्म से जुड़ी कुछ बातें
दो लफ्जों में
साल 2016 में आई ये किताब आपको ऑटिज्म के इतिहास के सफर पर ले जाती है। ऑटिज्म के पहले केस की पहचान से लेकर इसमें अब तक कौन कौन से मोड़ आए और आज भी इसके इलाज को लेकर मेडिकल कम्यूनिटी की अलग-अलग राय होती है ये सब आप इस किताब में पढ़ते हैं। ये किताब हमें ये भी बताती है कि ऑटिज्म से पीड़ित लोग भी अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और इस बीमारी की परेशानियों और कई अनसुलझे रहस्यों के बावजूद आने वाले कल में कोई अच्छी उम्मीद नजर आती है।
ये किताब किनको पढ़नी चाहिए?
• मानव अधिकारों और पब्लिक पॉलिसी में रुचि रखने वाले लोग
• चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी से जुड़े लोग
• ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के परिवार और दोस्त
लेखकों के बारे में
जॉन डोनवन, एबीसी न्यूज के लिए जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। उनको जाना माना एमी पुरस्कार मिल चुका है। उनकी पत्नी के परिवार में ऑटिज्म का केस होने की वजह से उनको इस विषय में बहुत रुचि है। कैरन जुकर भी जर्नलिस्ट हैं। इनको पी बॉडी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वे एबीसी के वर्ल्ड न्यूज और नाइटलाइन जैसे प्रोग्रामों की टीवी प्रोड्यूसर भी हैं। जब उनके बड़े बेटे में ऑटिज्म का पता चला तो कैरन की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। ये घटना इस किताब को लिखने की वजह भी बनी और उन्होंने ऑटिज्म पर एक सीरीज भी बनाई।
मानसिक बीमारियों के लेकर अमेरिकन मेडिकल कम्यूनिटी का रवैया कुछ खास अच्छा नहीं रहा है।
साल 2007 की बात है। न्यू जर्सी की एक बस में दो आदमियों ने एक ऑटिस्टिक किशोर को परेशान करना शुरू कर दिया। वो किशोर बार-बार एक सी हरकत कर रहा था। ये बात उन दोनों को अजीब लग रही थी। वे बार-बार उसे तंग करते। इसी वक्त बस में कोई दूसरा आदमी उठ खड़ा हुआ और उन दोनों को डांटते हुए कहा कि इस लड़के को ऑटिज्म है। आप दोनों इसे तंग न करें और चुप बैठें। इस घटना से ये पता चलता है कि आज भी ऑटिज्म के बारे में ज्यादातर लोग अनजान हैं और इस बीमारी से जूझ रहे लोग और उनके अपने, बाकी दुनिया की जागरूकता बढ़ाने के लिए कैसे लड़ रहे हैं। 1940 के दशक में पहली बार "ऑटिज्म" शब्द का इस्तेमाल किया गया। हालांकि तब से लेकर आज तक बहुत स्टडी और जानकारी हमारे पास इकट्ठी हो चुकी है। लेकिन उतनी ही इसका शिकार लोगों की गिनती भी बढ़ी है। इस किताब से पता चलता है कि समय के साथ ऑटिज्म के बारे में लोगों विचार कैसे बदले हैं और किन पहलुओं पर आज भी बहस होती है।
इस समरी को पढ़कर आप जानेंगे
• ऑटिज्म का शिकार पहला इंसान कौन था
• मूर्ख शब्द पहले मेडिकल डिक्शनरी में शामिल क्यों था
• ऑटिज्म और वैक्सीन के बीच क्या संबंध है
तो चलिए शुरू करते हैं!
हर समाज में मानसिक बीमारी को अलग नजरिए से देखा जाता रहा है। जैसे अगर रशिया की बात करें तो पंद्रहवीं सदी में ये माना जाता था कि ऐसी बीमारियां ईश्वर की देन हैं। इस तरह के लोगों को एक पवित्र मूर्ख के तौर पर देखा जाता था और उनका समाज उनकी रक्षा करता था। जबकि ये बीसवीं सदी के शुरुआती दौर में अमेरिकी समाज की सोच से काफी अलग है। इस दौरान वहां मानसिक रोगियों को "मेंटली डिफेक्टिव" कहा जाता था और इनकी सुरक्षा की जगह इनका शुद्धिकरण किया जाता था। ये शब्द डिफेक्टिव साल 1902 में बनाया गया था और इसे किसी भी तरह की दिमागी बीमारी वाले इंसान के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता था। फिर वो चाहे मिर्गी हो, डाउन सिंड्रोम, दिमाग की चोट या दिमाग की कोई भी और बीमारी हो। इन लोगों के इलाज का एक ही तरीका था कि इनको बाहरी दुनिया से दूर रखकर इलाज के लिए सेंटरों में भर्ती कर दिया जाए। भले ही आज की तारीख में हम डिफेक्टिव शब्द को बुरा मानते हों पर उस दौर में ये सिर्फ एक मेडिकल शब्द था जिसे आम लोगों से अलग बर्ताव करने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस दौरान ऐसे और भी कई शब्द इस्तेमाल किए जाने लगे थे। जैसे "इडियट" का मतलब था कि ऐसे किसी रोगी का दिमाग तीन साल से कम उम्र के किसी बच्चे जितना ही था। "imbecile" तीन से सात साल के बच्चे और "moron" सात से दस साल के बीच के बच्चे के बराबर दिमागी ताकत वाले इंसान को कहा जाता था। ऑटिज्म के इतिहास में एक और काला अध्याय था यूजीनिक्स आंदोलन।
यूजीनिक्स का मोटे तौर पर मतलब निकलता है अच्छी नस्ल पैदा करना। इसे सपोर्ट करने वालों का मानना था कि सिर्फ उन लोगों को ही बच्चे पैदा करना चाहिए जो पूरी तरह से फिट हैं ताकि आने वाली जेनरेशन में किसी तरह की जेनेटिक बीमारी न हो। किसी जेनेटिक या मानसिक बीमारी वाले इंसान को सामाज के लिए खतरे के तौर पर देखा जाता था क्योंकि इनसे पैदा हुए बच्चे खराब नस्ल के हो सकते हैं और इससे इंसानियत की शुद्धता खराब हो सकती है और उसका भविष्य भी। इसलिए बेहतर है कि ऐसी किसी संभावना को पहले ही खत्म कर दिया जाए। 1920 के दशक के दौरान बहुत से डॉक्टर और बायोलॉजिस्ट इस सोच का सपोर्ट किया करते थे। यहां तक कि थियोडोर रूजवेल्ट जैसे बड़े नेता भी इससे सहमत थे। इसे हार्वर्ड और येल जैसी यूनिवर्सिटीज और न्यूयॉर्क टाइम्स में जोर शोर से फैलाया गया और प्लान्ड पैरेंटहुड के फाउंडर मार्गरेट सेंगर जैसे सोशल एक्टिविस्ट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। इस समय के आसपास यूएस के 17 राज्यों ने जबरन नसबंदी को वैध कर दिया। कुछ ऐसे भी थे जो इसे एक कदम आगे ले जाना चाहते थे। 1942 में न्यूरोलॉजिस्ट रॉबर्ट फोस्टर कैनेडी ने अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने ऐसी बीमारियों को नेचर की गल्ती बताते हुए इसे मर्सी किलिंग से ठीक करने की बात कही।
डोनाल्ड ट्रिपलेट नाम के मरीज की वजह से ऑटिज्म को पहचाना जा सका।
ऑटिज्म के शिकार बच्चों के माता-पिता की परेशानी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक छोटा बच्चा जो बीमार है पर उसकी बीमारी को समझ पाना डॉक्टरों के लिए भी एक चुनौती है। साल 1933 में मिसीसिपी में रहने वाले मैरी और बीमन ट्रिपलेट नाम के कपल के घर डोनाल्ड नाम के बच्चे के पैदा होने के साथ ही मुश्किलें आ गईं। डोनाल्ड का बर्ताव शुरू से ही अजीबोगरीब था खास तौर पर जब बात लैंग्वेज की हो। डोनाल्ड 6 कहने की जगह hexagon कहता और "आप" की जगह "मैं" का इस्तेमाल करता। ज्यादा परेशानी तब नजर आने लगी जब डोनाल्ड ने बिना किसी वजह के "बिजनेस" "trumpet वाइन" और फूलों के नाम दोहराना शुरू कर दिया। लेकिन डोनाल्ड अपनी उम्र के बाकी बच्चों से बहुत आगे था। दो साल की उम्र में ही वो सारे अल्फाबेट्स सीधे और उल्टे बोल सकता था और किसी खिलौने को खोलकर उसे वैसे का वैसा फिट कर सकता था। उसके माता-पिता के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात ये थी कि वो भावनात्मक रूप से बहुत अलग था। ऐसा लगता था कि उसे अपने माता-पिता या किसी और की परवाह नहीं है। वो सबसे ज्यादा खुश तब होता था जब बस अपने आप में रहता था। उसे खिलौनों से खेलकर या बर्तनों के ढक्कन फर्श पर घुमाकर मजा आता था।
अगर कोई उसके कामों में रुकावट डाले तो डोनाल्ड हाथ पैर चलाने लगता था। उसे किसी भी तरह का बदलाव पसंद नहीं था फिर वो चाहे उसके रूटीन में हो या अपने आसपास के माहौल में। अफसोस की बात ये थी कि 1930 के दशक में डोनाल्ड की परेशानी को समझ पाने की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे लक्षणों के लिए कोई नाम तक नहीं था। डॉक्टर बस यही सलाह दे सकते थे कि उस समय चल रहे ट्रेंड का पालन करें। यानि किसी केयर सेंटर में भेज दें जहां उसकी देखभाल की जा सके। लेकिन ऐसे ही किसी सेंटर में एक साल बिताने के बाद भी डोनाल्ड में कोई बदलाव नहीं आया था। इसलिए उसे बाल्टीमोर के जानेमाने जॉन्स हॉपकिन्स अस्पताल में भर्ती करके डॉ लियो कनेर की देखरेख में रखा गया। अगले कुछ सालों में डॉ कनेर ने डोनाल्ड को बहुत गौर से देखा और इस अजीब सी कंडीशन के लिए डायग्नोसिस बनाना शुरू कर दिया।
बच्चों में ऑटिज्म के लिए उनकी मांओं को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता था।
साल 1943 में, कनेर ने "ऑटिस्टिक डिस्टर्बेंस ऑफ अफेक्टिव कॉन्टेक्ट" नाम का एक ऐसा पेपर पब्लिश किया जो मील का पत्थर साबित हुआ। इसे उन्होंने डोनाल्ड जैसे ग्यारह बच्चों की स्टडी करके लिखा था। अपनी स्टडी के बाद कनेर ने ऐसे लक्षणों के लिए एक नया शब्द दिया ऑटिज्म। इसमें तीन बातें जरूर पाई जाती थीं। पहला- बाकी लोगों से न मिलजुल पाना, अपने आप में या अकेले रहने की आदत और एक जैसे रूटीन की जिद। कनेर ने इस बात पर जोर दिया कि ये शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिनकी सेहत और दिमाग बहुत ज्यादा खराब न हुए हों। उनके पेपर में ये भी कहा गया कि ऑटिज्म को कोई नई घटना नहीं माना जाना चाहिए। इसकी जगह इसे ऐसी बीमारी कहा जाना चाहिए जिसे अब तक पहचाना नहीं जा सका था। इसके पीछे कनेर ने एक ऐसी थ्योरी को सामने रखा जो गलत होते हुए भी बहुत लोकप्रिय हो गई थी। इसे रेफ्रिजरेटर मदर थ्योरी कहा गया। इसमें कहा गया कि जो माएं अपने बच्चों से प्यार नहीं जतातीं या उनकी तरफ से लापरवाह होती हैं उनके बच्चे ऐसे हालात से बचने के लिए ऑटिस्टिक बन जाते हैं।
कनेर की थ्योरी को जल्द ही बहुत से लोगों का सपोर्ट मिल गया। इसमें शिकागो यूनिवर्सिटी के ऑर्थोजेनिक स्कूल के डायरेक्टर ब्रूनो बेटेलहेम भी शामिल थे। ये संस्था बच्चों के केयर सेंटर की तरह ही थी। लेकिन भले ही बेटेलहेम खुद को डॉक्टर कहने की जिद पर अड़े हों, वे लाइसेंस वाले डॉक्टर नहीं थे बल्कि उन्होंने आर्ट हिस्ट्री में पीएचडी की थी। लेकिन इसके बावजूद 1950 और 1960 के दशक के दौरान वे रेफ्रिजरेटर मदर थ्योरी के सबसे बड़े सपोर्टर थे और इसकी वकालत किया करते थे। मार्सिया नाम की एक ऑटिस्टिक बच्ची weather शब्द को लेकर डर जाती थी। उसके मामले में बेटेलहेम ने ये कह दिया कि वो इसलिए डर रही है कि कहीं उसकी माँ उसे खा न ले। क्योंकि इस शब्द को we/eat/her कहा जा सकता है। उनका ये दावा भी था कि इस अस्पताल में अपनी माँ से दूर रहकर उसका जो इलाज चल रहा था उसकी वजह से मार्सिया पूरी तरह ठीक हो रही थी।
ऑटिज्म के बारे में जागरुकता फैलाने में एक ऑटिस्टिक बच्चे के माता-पिता का बहुत बड़ा हाथ है।
ये कितने दुख की बात है कि कोई आपके बच्चे को छीनकर ले जाए और ऊपर से आपको ही गुनहगार ठहरा दे। लेकिन बेटेलहेम बिल्कुल यही कर रहा था। और इस बात का अंदाजा लगाना आसान है कि इसकी चपेट में आए माता-पिता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था।1960 के दशक में माता-पिता और कुछ एक्टिविस्ट इस सोच के खिलाफ एकजुट हो गए कि ऑटिज्म के पीछे गलत या लापरवाह पेरेंटिंग छिपी है और इसकी सही वजह पता लगानी चाहिए। रूथ सुलिवन आर्मी में नर्स का काम कर चुकी थीं। उनका बेटा भी ऑटिस्टिक था। पर वो इस गलत सोच के खिलाफ डटकर खड़े होने वालों में से एक थीं। उनके सात बच्चे थे। उनमें से जो नाम का एक ही बेटा ऑटिज्म का शिकार था। साल 1963 में वो जो को उन एक्सपर्ट्स को दिखाने के लिए ले गई, जिनको कनेर ट्रेनिंग दे चुके थे। लेकिन वहां भी उनको यही बताया गया कि वही अपने बेटे की बीमारी की वजह हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता था? एक ही घर में सात बच्चों की परवरिश हो पर सिर्फ एक पर ही असर पड़े? डॉक्टरों और नर्सों के पास सुलिवन के सवालों का कोई जवाब नहीं था। फिर भी उन्होंने सुलिवन से ये कहा कि वे ऑटिज्म से जुड़ी कोई किताब या जानकारी न पढ़ें वरना वो ज्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगी।
सुलिवन ने ये सलाह नहीं मानी और इसे तकदीर का लिखा मानकर चुप हो जाने की जगह नेशनल सोसाइटी फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन नाम की एक संस्था बना दी। इस संस्था ने पूरे यूएस में उन परिवारों को आपस में जुड़ने में मदद की जिनके घर ऑटिस्टिक बच्चे थे। सुलिवन ने मीडिया और कानून की मदद ली और इस बात के लिए अपील दायर की कि स्कूलों में ऑटिस्टिक बच्चों के लिए जगह बनाई जाए। उस समय स्कूलों के लिए मानसिक बीमारियों वाले बच्चों को ये कहकर एडमिशन से मना कर दिया जाता था कि वे पढ़ाई के लायक नहीं हैं। ये फैसला कानून के दायरे में आता था। लेकिन सुलिवन को पता था कि उसे क्या करना है। उसने क्लासरूम में ज्यादा टीचरों और अटेंडेंट को बुलाने की मांग की ताकि ऑटिस्टिक बच्चों की सही देखभाल की जा सके। 1960 के दशक में सुलिवन ने बड़े अधिकारियों, राजनेताओं और रिसर्चर्स के साथ जुड़ना शुरू किया और धीरे-धीरे ऑटिस्टिक बच्चों से होने वाला भेदभाव, उनके लिए एक्सेप्टेंस में बदलने लगा। आगे चलकर सुलिवन ने साइकोलॉजिस्ट डॉ बर्नार्ड रिमलैंड के साथ काम किया जिन्होंने रेफ्रिजरेटर मदर थ्योरी की गलती को पहचाना। उन्होंने कहा कि इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई वैज्ञानिक डेटा या सबूत नहीं था।
ऑटिज्म को लेकर गलत और गुमराह करने वाली थ्योरीज दी जाती रही हैं।
एक्टिविस्ट्स अपनी तरफ से काफी बदलाव ले आए लेकिन इस जीत के बावजूद ऑटिज्म से प्रभावित परिवारों और लोगों के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। 1960 के दशक में साइकोलॉजी की फील्ड में एप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस (ABA) बढ़ रहा था। इसे एक नॉर्वेजियन-अमेरिकी मनोवैज्ञानिक इवर लोवास ने दुनिया के सामने रखा था जिसने ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बहुत गलत तरीके के इलाज की वकालत की। जैसे कि इलेक्ट्रोथेरेपी, डांट फटकार और पिटाई। लोवास का मानना था कि इन तरीकों से बच्चों को "सामान्य" बर्ताव करने लगेंगे और ऑटिस्टिक रवैया छोड़ने को राजी हो जाएंगे। पिछले कुछ सालों में ABA ने one-on-one थेरेपी सेशन्स को शामिल किया है। इसमें सोशल स्किल बढ़ाने और अच्छे बर्ताव पर रिवार्ड देने जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। ये इलाज काफी लोकप्रिय है। इसका सपोर्ट करने वालों का मानना है कि एबीए ऑटिस्टिक बच्चों को बेहतर बनाने और बदलने में मदद करता है।
हालांकि इसके खिलाफ खड़े लोगों का कहना है कि एबीए और कुछ नहीं बल्कि डॉग ट्रेनिंग का इंसानी रूप है। वे इसकी जरूरत पर सवाल उठाते हैं। इनका कहना है कि ये सब ऑटिस्टिक बच्चों को नॉर्मल दिखाने का एक तरीका भर है। ऑटिज्म के बारे में हाल में एक और अफवाह चली है कि वेक्सीनेशन और ऑटिज्म के बीच संबंध है। पिछले दो दशकों में ऑटिज्म की बढ़ती संख्या को देखकर कुछ लोगों ने इसे महामारी का नाम दे दिया है। साल 1998 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एंड्रयू वेकफील्ड ने लैंसेट मैग्जीन में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने खसरा, mumps और रूबेला से बचाव के लिए दी जाने वाली MMR वैक्सीन को ऑटिज्म से जोड़ दिया। हालांकि वेकफील्ड का आर्टिकल रिसर्च पर आधारित था लेकिन बाद में कोई भी स्टडी इसे साबित नहीं कर सकी। इस वजह से उनके दावे को खारिज कर दिया गया। इस वजह से साल 2010 में ये आर्टिकल हटा लिया गया और यूके जनरल मेडिकल काउंसिल ने वेकफील्ड का मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया। फिर भी ऐसे कई बड़े नाम हैं जो आज भी इस थ्योरी का सपोर्ट करते हैं।
आज भी ऑटिज्म की कोई सटीक परिभाषा या सबसे अच्छा इलाज तय नहीं हो पाया है।
कई लोगों को ऑटिज्म और उससे जुड़ी मुश्किलों की जानकारी साल 1988 में आई फिल्म रेन मैन से मिली जिसमें डस्टिन हॉफमैन ने एक ऑटिस्टिक लेकिन बहुत समझदार इंसान और टॉम क्रूज ने उनके भाई की भूमिका निभाई है जो अपने भाई से परेशान तो है पर उसे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव भी है। इस फिल्म ने ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इससे पहले कि हम कुछ कर सकें हमें पहले एक जैसी सोच बनाने की जरूरत है। यहां मुश्किल ये आ जाती है कि ऑटिज्म में बहुत सी कंडीशन्स होती हैं। इसलिए एक जैसा इलाज सबको नहीं दिया जा सकता।
एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो बातचीत या अपना ध्यान तक नहीं रख सकते। वो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ऑटिज्म कोई रुकावट नहीं है। ये लोग अच्छी तरह से बोल सकते हैं, अपनी देखभाल कर सकते हैं। इनके लिए ऑटिस्टिक होना एक खास पहचान है। इन लोगों में इतना टैलेंट है कि इनका इलाज करने की जगह इनको सम्मान दिया जाना चाहिए। इनके कुछ गुण तो तारीफ के काबिल होते हैं। जैसे कुछ ऑटिस्टिक लोगों को तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। जबकि कुछ लोग रेन मैन के हॉफमैन की तरह बहुत समझदार हैं। जैसे वो ईंटों की दीवार को देखकर तुरंत ये बता सकते हैं कि इसमें कितनी ईंटें लगी हैं।
ऑटिज्म को पहचानने में इतनी मुश्किल इसलिए आती है क्योंकि इसे ब्लड या स्वैब टेस्ट से पकड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है या फिर किसी ऐसे एक्सपर्ट की जो ये समझ सके कि उसे क्या पता लगाना है। ये तो तय है कि ऑटिज्म के लिए और ज्यादा समझ और खुले दिमाग की जरूरत है। इस एक बात पर हम सभी शायद सहमत हो सकते हैं कि ऐसे लोगों के साथ बुरा बर्ताव रोकना चाहिए। हालांकि हम ऑटिज्म को पूरी तरह से नहीं समझते हैं और शायद ही कभी इसकी कोई एक परिभाषा बन पाए। फिर भी हम अपना दिल बड़ा कर सकते हैं और एक बेहतर कल की बुनियाद रख सकते हैं।
कुल मिलाकर
ऑटिज्म का एक लंबा और काला इतिहास है जो आज भी रहस्य बना हुआ है। एक समय पर इसे मानव जाति के ऊपर किसी कलंक की तरह देखा जाता था या फिर माताओं की लापरवाही या टीके लगवाने के नुकसान के रूप में। लेकिन आज ऑटिज्म को लेकर काफी जानकारी जुटाई जा रही है जिसकी वजह से इसे समझना आसान हो जाता है। साल दर साल हम और जागरूक होते जा रहे हैं। लेकिन इस बारे में अभी भी बहस चल रही है कि इसके पीछे क्या वजह है और इसका सबसे अच्छा इलाज क्या हो सकता है।
येबुक एप पर आप सुन रहे थे In a Different Key By John Donvan and Caren Zucker.
ये समरी आप को कैसी लगी हमें yebook.in@gmail.com पर ईमेल करके ज़रूर बताइये.
आप और कौनसी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं. हम आप की बताई गई समरी एड करने की पूरी कोशिश करेंगे.
अगर आप का कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें ईमेल करके ज़रूर बताएं.
और गूगल प्ले स्टोर पर ५ स्टार रेटिंग दे कर अपना प्यार बनाएं रखें.
Keep reading, keep learning, keep growing.