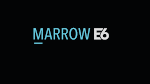Paul Hawken (ed.)
ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के तरीके
दो लफ्जों में
ग्लोबल वार्मिंग आज के दौर की सच्चाई है और इसकी सबसे बड़ी वजह इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से रिलीज होने वाला कार्बन है। ये किताब आपको बताती है कि भले ही लोगों ने कितनी तबाही मचा रखी हो पर अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। सोलर पावर, एग्रो फॉरेस्ट्री और इलेक्ट्रिक कार जैसे ढेरों उदाहरण लेकर ये किताब बताती है कि किस तरह कार्बन रिलीज को बहुत कम किया जा सकता है। इसमें हर वो तकनीक और तरीका बताया गया है जिसकी मदद से ग्लोबल वार्मिंग कम करके दुनिया को बचाया जा सकता है।
ये किताब किनको पढ़नी चाहिए?
• हर वो इंसान जो आने वाले कल की परवाह करता है
• समाज के ऊंचे पायदान पर खड़े लोग
• साइंस और नेचर से लगाव रखने वाले लोग
इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे
• वेजिटेरियन खाना किस तरह धरती को बचाने में मदद कर सकता है
• घरों में इस्तेमाल होने वाली कौन सी चीज ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी वजह है
• गाय और पेड़ों में क्या समानता है
लेखक के बारे में
प्रोजेक्ट Drawdown में ऐसे वैज्ञानिक, एक्टिविस्ट और नेता शामिल हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कम करने से जुड़े कामों में जी जान से लगे हैं। इसमें एनवायरमेंट के लिए काम करने वाले Bill McKibben, Peter Wohlleben, Tom Brady और Gi1sele Bündchen जैसे जाने माने नाम शामिल हैं। पॉल एक जर्नलिस्ट और entrepreneur हैं और इस प्रोजेक्ट के को फाउंडर हैं।
ग्लोबल वार्मिंग को बदला जा सकता है।
अगर आप धरती की जरा भी परवाह करते हैं तो आपको ग्लोबल वार्मिंग की खबरें चिंता में डाल देती होंगी। इसका असर वैज्ञानिकों के अंदाजे से कहीं तेजी से दिखने लगा है। साल दर साल बढ़ती गर्मी हो या समुद्रों में बढ़ता एसिड लेवल, जंगलों में लगने वाली आग हो या पोल्स पर पिघलती बर्फ हर जगह बस तबाही के आसार दिखते हैं। इसके बावजूद भी कार्बन डाई ऑक्साइड का रिलीज बढ़ता ही जा रहा है। प्रोजेक्ट Drawdown ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो इन हालात को बदलने के लिए कमर कसे हुए हैं। रिसर्च और स्टडीज को बुनियाद बनाकर ये इस काम पर लगे हुए हैं कि कैसे कम से कम खर्चे में कार्बन डाई ऑक्साइड रिलीज को घटाया जाए। इस किताब में कुछ ऐसे पक्के उपाय दिए गए हैं जहां लोग पर्सनल लेवल पर, एक ग्रुप के तौर पर या समाज के तौर पर अपनी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बिजनेस और सरकार से जुड़े लोग और पॉलिसी बनाने वालों के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। Renewable energy जैसे तरीकों से लेकर कबीलों और आदिवासियों को बसाने तक ऐसे बहुत से रास्ते हैं जो मंजिल तक ले जा सकते हैं। इससे ना सिर्फ धरती का भला होगा बल्कि इंसानों की सेहत और पैसों का फायदा भी मिलेगा।
अपने दौर के जाने माने स्कॉलर Alexander von Humboldt जब साल 1829 में रशिया से गुजरे तब वहां का हाल देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि किस तरह अंधाधुंध खेती की वजह से वो खूबसूरत जगह बर्बाद हो गई थी। वो उन पहले वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि इंसान, एनवायरमेंट पर किस तरह से बुरा असर डाल सकते हैं। उन्होंने ही ये बताया था कि जंगलों का सफाया और फैक्ट्रियों से निकली जहरीली गैसें एनवायरमेंट के लिए दो सबसे बड़े खतरे हैं। इसके लगभग 150 सालों बाद 1975 में वॉलेस ब्रोएकर नाम के जीओलॉजिस्ट ने ग्लोबल वार्मिंग नाम का शब्द दुनिया के सामने रखा जिसका मतलब था धरती का तापमान लगातार बढ़ते जाना। आज हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हकीकत है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि ये सदी खत्म होते होते धरती का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका होगा। इस बदलाव की वजह से जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती हैं, सूखा पड़ता है, समुद्रों का लेवल बढ़ जाता है और इन सबकी वजह से तबाही आती है। लोग भी बड़ी तादाद में माइग्रेट करते हैं। Humboldt ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि इसकी क्या वजह है। इंसान अपनी घरेलू या कामकाजी जरूरतों के लिए कोयला और पेट्रोलियम जैसे फ्यूल जलाते हैं। सीमेंट और कांक्रीट के जंगल बसाते हैं और गलत तरीकों से खेती करके जमीन, हवा और पानी को चौपट कर रहे हैं। इन सबकी वजह से कार्बन डाई ऑक्साइड और कुछ दूसरी नुकसानदायक गैसें रिलीज होती है। जिसे ग्रीनहाउस इफेक्ट कहा जाता है। इसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ता है।
ये जानते हुए भी कि कार्बन रिलीज होने का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में कितना बड़ा हाथ है इसका लेवल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। 2016 में 36 गीगाटन कार्बन डाई ऑक्साइड रिलीज हुई थी। ये साइज के हिसाब से 4 लाख ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर होगा। इस तरह तो कार्बन रिलीज घटाकर भी कुछ नहीं बदलेगा। हमें इसे पूरी तरह बंद ही करना होगा। लेकिन इसके साथ कुछ और तरीकों को बढ़ावा भी देना होगा। जैसे पौधों का अपना फोटोसिंथेसिस जिससे ऑक्सीजन बढ़ती है और कार्बन डाई ऑक्साइड कम होती है। राहत की बात ये है कि ग्लोबल वार्मिंग को बदलने के तरीके हमारे पास पहले से मौजूद हैं। जैसे renewable एनर्जी, जंगलों को बचाना और sustainable फार्मिंग। बदलती तकनीकें जैसे e-cars, ocean farming और carbon air capture भी ढूंढ लिए गए हैं। इनके और भी काफी फायदे हैं। पैसे की बचत होती है, रोजगार के नए मौके बनते हैं, प्रदूषण घटता है और लोगों की सेहत भी सही रहती है। अब इनके फायदे डीटेल में समझते हैं।
फॉसिल फ्यूल की जगह सोलर, हाइड्रो और विंड एनर्जी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
घरों में जलने वाली लाइट के लिए बिजली कहां से आती है? इस बात की संभावना ज्यादा है कि इसके लिए कोयला या फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया गया होगा। दुनिया में आज भी लगभग 80% बिजली के लिए कोयला, गैस या तेल ही जलाया जाता है। इन सबमें भरपूर कार्बन होती है। लेकिन अगर हम सच में ग्लोबल वार्मिंग के खतरों की चिंता करते हैं तो इस तरीके को बदलना होगा। एनर्जी तो हमारे चारों तरफ भरी हुई है। सूरज की रोशनी, हवा, पानी इन सबमें एनर्जी है। अब ऐसी तकनीकें भी बढ़ती जा रही हैं जिनकी मदद से एनर्जी बनाना आसान होता जा रहा है। विंड एनर्जी को इनका मुखिया कहा जा सकता है। विंड फार्म बनाना काफी सस्ता भी है और इनकी एफिशिएंसी भी बहुत होती है। जैसे लिवरपूल में लगी विंड 32 टरबाइनों में से कोई एक भी अगर एक चक्कर पूरा कर लेती है तो इतनी बिजली बन जाती है कि एक घर का रोजाना का काम चल जाए। डेनमार्क पहले ही बिजली की लगभग 40% जरूरत विंड एनर्जी से पूरी कर रहा है। अगर दूसरे देश भी इसी रास्ते पर चलने लगें तो साल 2050 आते आते इनकी लगभग 21.6% जरूरत पूरी हो सकती है। इसकी वजह से 84.6 गीगाटन कार्बन डाई ऑक्साइड कम रिलीज होगी। इसी तरह सोलर एनर्जी भी हर साल 330 मिलियन कार्बन डाई ऑक्साइड का रिलीज बचा रही है।
सोलर पैनल, सूरज की किरणों में मौजूद फोटॉन से एनर्जी जनरेट करते हैं। इनको छोटे लेवल पर घर की छतों में भी लगाया जा सकता है और इकट्ठा करके बड़े सोलर फार्मों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी भी दुनियाभर में 1 बिलियन से ज्यादा लोग इनकी मदद से अपनी बिजली की जरूरत पूरी कर रहे हैं। खास तौर पर ऐसे लोग जिनके पास बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। लेकिन एनर्जी स्टोर करना और उसे घरों या बिल्डिंगों तक पहुंचाना भी एक चैलेंज है। अभी जितनी भी एनर्जी बनती है उसमें से एक बड़ा हिस्सा तो हीट में बदलकर खराब हो जाता है। ऐसे सिस्टम बनाए जा सकते हैं जो इस हीट का भी इस्तेमाल कर लें। इको फ्रेंडली एनर्जी के लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और फाइनेंशियल मदद की जरूरत होगी। साल 2015 में ग्लोबल फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को सब्सिडी के तौर पर 5.3 ट्रिलियन मिले थे। अगर यही पैसा renewable energy की फील्ड में लगाया जाए तो कितना भला हो सकता है।
हमें मीट की खपत कम करने, खेती के अच्छे तरीके अपनाने और खाने की बर्बादी घटाने की जरूरत है।
बुद्ध, कन्फ्यूशियस और लियोनार्डो दा विंसी में कौन सी बात एक जैसी थी? ये तीनों प्लांट बेस डाइट को सपोर्ट करते थे। पुराने जमाने की हर अच्छी आदत अब खत्म होती जा रही है। अब लोग पहले से कहीं ज्यादा मीट खा रहे हैं। 20% ग्रीनहाउस गैसें तो मीट इंडस्ट्री की वजह से ही रिलीज हो रही हैं। इसमें जानवर पालना तो शामिल है ही पर वो खेती भी शामिल है जो उनको पालने के लिए करनी पड़ती है। इस परेशानी का हल तो बहुत आसान है कि आप मीट की खपत कम कर दें। वेजिटेरियन या प्लांट बेस डाइट पर जोर दें तो भोजन से होने वाला कार्बन रिलीज 63% कम किया जा सकता है। इसके लिए लोगों को अवेयर बनाने के कैंपेन चलाए जा सकते हैं। अगर आधी दुनिया तक भी ये मैसेज चला गया तो कार्बन रिलीज 2050 तक 66 गीगाटन कम किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ भोजन की आदत बदलना काफी नहीं होगा। इसे पैदा करने का तरीका भी बदलना होगा। मॉडर्न एग्रीकल्चर इस पैटर्न पर काम करता है कि हर साल एक ही तरह की फसल उगाई जाए जब तक जमीन का न्यूट्रीशन पूरी तरह खत्म न हो जाए। पर इसकी वजह से जमीन में बंधी कार्बन भी हवा में मिल जाती है।
जबकि एग्रोफॉरेस्ट्री जैसी तकनीकें जमीन को और ज्यादा उपजाऊ बनाती हैं और कम कार्बन रिलीज करती हैं। इसमें पौधे और जानवर एक दूसरे को बेनिफिट करते हुए फलते फूलते हैं। स्पेन और पुर्तगाल में ये सिस्टम बहुत पहले से चल रहा है। इसे silvopasture agroforestry सिस्टम कहा जाता है। इसमें गायों को खेतों की जगह जंगलों में चरने के लिए छोड़ा जाता है। पेड़ों की वजह से इनको छाया तो मिलती ही है लेकिन ये पेड़, कार्बन को भी सोख लेते हैं। इस वजह से जानवरों से रिलीज हुई मीथेन का बैलेंस बन जाता है। अगर दुनिया में इन गायों को 60% भी बढ़ा दिया जाता है तो 2050 तक कार्बन रिलीज 31.1 गीगाटन कम हो जाएगा। हम क्या खाते हैं उतना ही मायने ये भी रखता है कि हम क्या नहीं खाते। दुनिया के 800 मिलियन लोग अभी भी भूख का शिकार हैं लेकिन दुनिया में पैदा होने वाले अनाज का तीसरा हिस्सा कभी किसी को मिलता ही नहीं है। बड़े देशों में अगर व्यापारियों को फसल की क्वालिटी में जरा भी अंतर दिखा यानि दानों का आकार या मामूली सी टूट फूट तो वो फसल लेने से मना कर देते हैं। अगर सुपर मार्केट में कोई फल सब्जी ना बिकी तो वो उसे फेंक देते हैं। बेस्ट बिफोर का भी कोई सही नियम नहीं है। खराब क्वालिटी की फसल उगाना तो गलत है पर उगाई गई हर चीज को खराब बोलकर फेंक देना भी तो सही नहीं है। लेकिन अगर खाने की बर्बादी 50% भी कम कर दी जाए तो साल 2050 तक 26.2 गीगाटन कार्बन रिलीज घट सकता है।
शहरों को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे एनर्जी की बचत हो।
जगह-जगह फैला धुआं, ट्रैफिक जाम और हरियाली की कमी किसी भी शहर को नेचर के दुश्मन के तौर पर दिखाने के लिए काफी है। लेकिन यही ठसाठस बसी आबादी इस बात पर जोर दे सकती है कि पानी, एनर्जी और बिजली के लिए इको फ्रेंडली तरीके इस्तेमाल किए जाएं। इसमें सबसे पहला कदम होगा ऐसी बिल्डिंगे बनाना जो ज्यादा से ज्यादा energy-efficient हों। दीवारें और छतें फाइबर ग्लास या अखबारों से बनाई जाएं तो मकान सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। इस तरह हीटर या एयर कंडीशनर की जरूरत अपने आप कम हो जाएगी। छतों पर पौधे लगाने से बिल्डिंग ठंडी भी रहेगी और कार्बन भी घटेगा। अब ऐसे शीशे भी आ गए हैं जो वक्त या रोशनी के हिसाब से अपना रंग बदल लेते हैं। इनको electrochromic glass कहा जाता है। इस तरह भी कमरों का तापमान सही बना रहता है। इस तरह की तकनीकों से बिजली की खपत तो कम होती ही है पर एनवायरमेंट पर भी अच्छा असर पड़ता है। जैसे अगर हर बिल्डिंग में energy-friendly LED लाइट बल्ब लगाना शुरू हो जाए तो साल 2050 तक कार्बन रिलीज 12.8 गीगाटन घट सकता है।
पर इन सबको लागू करना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए हमें सबसे पहले हर नई बिल्डिंग के लिए ये नियम बनाने होंगे। पुरानी बिल्डिंगों में भी बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की 6541 खिड़कियों में इन्सुलेटर लगाकर यहां एनर्जी की खपत को 40% कम कर दिया गया। क्लाइमेट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देकर भी शहरों का रूप बदला जा सकता है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल और पैदल चलने को बढ़ावा देना। अगर शहरों में घर, दुकानों, कैफे और पार्कों के आसपास ऐसी पतली सड़कें बना दी जाएं जहां पैदल चलना या साइकिल चलाना आसान हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग इनको इस्तेमाल करेंगे। कारों का इस्तेमाल घटेगा। लोग हेल्दी भी रहेंगे और पैसों की बचत भी कर पाएंगे। नीदरलैंड्स में ऐसी सड़कों की भरमार है। इसलिए इसे दुनिया के सबसे ज्यादा bike-friendly देशों में गिना जाता है। यहां लगभग 27% कामों के लिए लोग साइकिल ही इस्तेमाल करते हैं। अगर दुनिया में ये आंकड़ा 7.5% भी हो जाए तो साल 2050 तक कार्बन रिलीज 2.31 गीगाटन तक कम हो सकता है। शहरों की तरफ आती हुई आबादी को तो कंट्रोल किया ही जा सकता है। इसके साथ इनको मिलने वाली बिजली, पानी और एनर्जी को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। अगर सबके लिए कॉमन पावर ग्रिड्स ही लग जाएं तो ओवर प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट में होने वाला नुकसान भी कम हो सकता है। कोपनहेगन में यही किया गया है। इसे पावर प्लांट से निकलने वाले वेस्ट से चलाया जाता है जिससे लोगों के घरों में लगे हीटिंग सिस्टम जुड़े हैं। आज दुनिया के बस 0.1% हिस्से में ये किया जा रहा है। अगर यही उपाय 10% शहर भी अपना लें तो साल 2050 तक कार्बन रिलीज 9.38 गीगाटन तक कम हो सकता है।
गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा fuel-efficient और climate-friendly बनाने की जरूरत है।
सभ्यता की शुरुआत से इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा है। कभी घूमने, कभी काम की तलाश तो कभी बसने के लिए हम दुनियाभर में घूमते रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम जिन कार, बसों, रेलों या जहाजों पर निर्भर करते हैं उनमें ज्यादातर फॉसिल फ्यूल की मदद से ही चलते हैं। पानी के जहाज या ट्रक भी इनसे अलग नहीं हैं। इनसे निकलने वाली कार्बन कम करने के लिए इनमें बदलाव की जरूरत है। जैसे डिजाइन, मेंटेनेंस और तकनीक पर काम करना। इनकी समय समय पर जाँच भी करते रहना चाहिए। इस तरह फ्यूल की खपत सही बनी रहेगी और कार्बन रिलीज घटेगा। अभी हवाई जहाजों से दुनिया में होने वाले कार्बन रिलीज का लगभग 2.5% हिस्सा बनता है। जैसे जैसे हवाई जहाज में सफर करने वाले लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसमें और बढ़त ही होगी। इससे निपटने के लिए बोइंग और नासा इस तरह के प्लेन बनाने पर काम कर रहे हैं जो बाकियों से लगभग 50% तक fuel-efficient हों। इसमें इंजन पीछे की तरफ लगा होगा और इसके पंख हल्के होंगे। इसकी वजह से प्लेन का वजन कम होगा और ये हवा में ज्यादा आसानी से उड़ पाएगा। पानी के जहाजों से होने वाले प्रदूषण को अक्सर नजर अंदाज कर दिया जाता है जबकि इनकी वजह टोटल कार्बन रिलीज का लगभग 3% हिस्सा आता है। अगर इनकी स्पीड में थोड़ी कमी कर दी जाए तो भी फ्यूल की खपत काफी कम हो सकती है।
लेकिन हवाई या पानी के जहाज भी एक साल में उतना कार्बन रिलीज नहीं करते जितना कार, ट्रक और बसें करती हैं। ये कुल कार्बन रिलीज का लगभग 25% हिस्सा बनाते हैं। अगर इनके इंजन का साइज या गाड़ियों का वजन कम कर दिया जाए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सही कदम तो ये होगा कि इनकी जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन इनके पूरी तरह तैयार होने तक हाइब्रिड गाड़ियां भी बनाई जा सकती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और फ्यूल दोनों तरह के इंजन लगे होते हैं। ये बाकी कारों की तुलना में लगभग 30% fuel-efficient होती हैं। अब बहुत से देशों की सरकारें इनको बढ़ावा देने के लिए इन पर सब्सिडी दे रही हैं। इसके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ाया जाना चाहिए। यानि बसें, मेट्रो और रेल सर्विस। इस तरह का ट्रांसपोर्ट सस्ता भी होता है और आसान भी। ट्रैफिक की परेशानी भी दूर होती है और प्रदूषण भी कम फैलता है। गाड़ी पूल करना, ई बाइक और ई स्कूटर भी अच्छा विकल्प हो सकते हैं। इसके लिए मोबाइल एप भी आ गए हैं। इससे लोगों के लिए ऐसी सर्विस लेना आसान हो गया है।
हमें जंगल, जमीन, पानी और मिट्टी को बचाने की जरूरत है।
अभी तक हमने क्लाइमेट चेंज की परेशानी का एक तरफ से हल सोचा है यानि कार्बन रिलीज कम कर देना। लेकिन अब हम दूसरे पहलू पर भी बात करेंगे। यानि कार्बन तो कम करना है पर बढ़ाना क्या है। हमें उस इकोसिस्टम को बढ़ाना है जो कार्बन को सोखकर वापस जमीन में भेज दे जो उसकी असली जगह है। जंगल और खास तौर पर रेन फॉरेस्ट का इको सिस्टम काफी डायवर्ट होता है। यहां पौधे, पेड़, कीड़े मकोड़े, और तरह तरह के जानवर एक इकोसिस्टम बनाकर रहते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि पेड़ भी अपना नेटवर्क बनाकर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसमें फंगस उनकी मदद करते हैं। इसे "wood wide web" का नाम दिया गया है। इसकी मदद से वो आपस में न्यूट्रीशन, insects, सूखा और दूसरे खतरों की जानकारी बांटते हैं। जंगलों ने करीब 300 बिलियन टन कार्बन सोख रखी है। इसके बाद भी हर साल 15 बिलियन पेड़ काट दिए जाते हैं। इसकी वजह से जमीन तो खराब होती ही है पर जमीन में बंधी हुई कार्बन भी हवा में मिल जाती है। हर साल टोटल कार्बन रिलीज का लगभग दसवां हिस्सा ऐसे ही आता है। जंगलों की कटाई तुरंत रोकनी चाहिए। ब्राजील में चलाए जाने वाले forest protection आंदोलन से सबक लिया जा सकता है। यहां 2004 में सख्त कदम उठाकर जंगलों की कटाई पर रोक लगाई गई थी। जमीन के साथ साथ सेटेलाइट की मदद से भी निगरानी रखी जाती थी कि कोई पेड़ या जंगलों को नुकसान ना पहुंचाए। जंगल बचाने के लिए फंडिंग की गई। इस वजह से और जंगल कटना तो बंद हो ही गए पर पहले से काटे जा चुके जंगलों को भी बसाया जा सका।
ज्यादातर जंगलों को फिर से बसाना कोई बड़ी मेहनत का काम नहीं होता। अगर जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये फिर से हरी भरी होने लगती है। इस तरह साल 2050 तक लगभग 235 मिलियन एकड़ जंगलों को वापस बसाया जा सकता है। यानि कार्बन रिलीज 22.61 गीगाटन कम हो सकती है। एक और तरीका है कि खाली जमीन में तरह-तरह के बीज लगा दिए जाएं।
हमें पानी के किनारों के आसपास की जमीन यानि कोस्टल इलाकों पर भी ध्यान देना होगा। इसमें marshes, meadows, mangroves और peatlands जैसे कि bogs and mires शामिल हैं। Peatlands तो कार्बन का भंडार होते हैं। ये पेड़ पौधों के सड़ने गलने से बनते हैं और इनमें जंगलों से दो गुनी ज्यादा कार्बन सोखने की ताकत होती है। हमें इनको बचाए रखने पर काम करना चाहिए। किसी इलाके के मूलनिवासी लोगों पर ही क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर पड़ता है लेकिन इसमें उनकी जिम्मेदारी सबसे कम होती है। ऐसे लोग इकोसिस्टम को बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इनका अपना रहन सहन और तौर तरीके काफी इको फ्रेंडली होते हैं। ऊपर से ये नेचर को बचाने की हर तरह से कोशिश भी करते हैं। इनका खेती और जानवर पालने का तरीका भी ऐसा होता है कि नेचुरल रिसोर्स खराब होने की जगह और बढ़ें। इनकी मदद लेकर हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन इनको पूरी भागीदारी देनी होगी। इनकी जमीन इनको वापस दी जाए और दूसरी जगह माइग्रेट कर चुके लोगों को वापस बसाया जाए।
हमें रीसाइक्लिंग की आदत डालनी होगी।
घरों में इस्तेमाल होने वाली एक चीज ने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जिसे लगभग हर घर में इस्तेमाल किया जाता है और वो है आपका रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनरों में जो कूलिंग मटेरियल डाला जाता है वो एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी एक यूनिट, कार्बन डाई ऑक्साइड के एक molecule से 9000 गुना ज्यादा हीट रिलीज करती है। इस समय जो केमिकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है hydrofluorocarbon या HFC. साल 2016 में हुई एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 170 देश इस बात पर सहमत हुए थे कि इन पर 2024 तक पूरी तरह रोक लगा दी जाए। लेकिन इसके खतरे देखते हुए इस काम के लिए बहुत मेहनत और निगरानी की जरूरत है। फिर भी अगर हम सही तरह इनको दूर कर पाते हैं तो 2050 तक कार्बन रिलीज में 90 गीगाटन की कमी आ सकती है। यानि क्लाइमेट चेंज पर सबसे बड़ा पॉजिटिव कदम यही होगा। वैज्ञानिकों के हिसाब से अकेले इस कदम से तापमान में एक डिग्री फैरनहाइट की कमी आ सकती है। लेकिन रोजमर्रा में लगने वाली सीमेंट और प्लास्टिक जैसी चीजें भी बदलनी चाहिए।
सीमेंट बनाने के लिए चूने के पत्थर को decarbonization प्रोसेस से गुजारा जाता है पर अपने नाम से उलट इस तरीके में बहुत कार्बन रिलीज होती है। एक उपाय है कि कोयला जलने से बची फ्लाई ऐश से सीमेंट बनाई जाए। इस प्रोसेस में decarbonization की जरूरत नहीं पड़ती है। यानि कार्बन रिलीज भी कम। प्लास्टिक बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल की जगह खाने या पेपर के वेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जब कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल हो चुका होता है तो उसका क्या करना है। सबसे आम तरीका तो ये है कि इसे रीसाइकल कर लिया जाए। कागज, कपड़े, गत्ते के डिब्बे, मेटल, लकड़ी या फूड वेस्ट हर चीज को रीसाइकल किया जा सकता है। इनसे खाद या बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। सरकार पॉलिसी बनाकर भी रीसाइकल को बढ़ावा दे सकती है। जैसे सैन फ्रांसिस्को में कचरा उठवाने के लिए तो पैसे देने पड़ते हैं पर रीसाइकल के लिए कुछ देना हो तो वो फ्री में कैरी कर लिया जाता है।
लोगों में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है।
पॉलिसी बनाना, उनको सही तरह लागू करना और सब्सिडी देना तो सरकारों, संस्थाओं और कॉर्पोरेट सेक्टर्स का काम है लेकिन हम भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। कैंपेन चलाकर, एक दूसरे को समझाकर और encourage करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहां किसानों की बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि sustainable फार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कम करने में बहुत मदद कर सकती है। अब NGO भी किसानों को इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। चावल उगाने की एक तकनीक है जिसे SRI यानि System of Rice Intensification कहा जाता है। चावल पूरी दुनिया में खाया जाता है। वैसे तो चावल की खेती में बहुत पानी लगता है पर इस तकनीक में धान जल्दी बो दिया जाता है, पानी की बचत की जाती है और केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पैदावार भी अच्छी होती है और ग्रीनहाउस गैसें भी कम रिलीज होती हैं। SRI का अलग से कोई खर्चा भी नहीं आता। लेकिन किसानों को बदलाव के लिए तैयार करना इतना आसान भी नहीं होता है। इसलिए SRI तकनीक एक से दूसरे किसान को सिखाई गई। इस तरह की ट्रेनिंग में महिला किसानों को भी जरूर जोड़ना चाहिए। भले ही खेती के काम से जुड़े लोगों में 43% महिलाएं होने के बावजूद भी उनको वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार हैं।
पैसे, शिक्षा या रिसोर्स की कमी की वजह से उनका काम पीछे जरूर रह जाता है। उनको पैसों की मदद करके और sustainable फार्मिंग के तरीके सिखाकर ये गड़बड़ ठीक की जा सकती है। लेकिन सिर्फ महिला किसानों ही नहीं दूसरी महिलाओं को भी जागरूक बनाना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा एक बहुत जरूरी मुद्दा है। एक तो पढ़ी लिखी महिलाएं बच्चे कम पैदा करती हैं। हालांकि आबादी और क्लाइमेट चेंज के कनेक्शन पर हमेशा विवाद होता है। फिर भी हर महिला ये चाहती है कि उसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अच्छी सर्विस मिले। एक सर्वे में गरीब तबके की 240 मिलियन महिलाओं ने कहा कि वो इस बात का फैसला खुद करना चाहती हैं कि उनको बच्चे कब पैदा करने हैं। अगर इनको फैमिली प्लानिंग का मौका या सुविधा मिले तो इनकी लाइफ तो सुधरेगी ही और आबादी भी कंट्रोल में रहेगी। इससे कार्बन डाई ऑक्साइड रिलीज में भी कमी आएगी।
सेल्फ ड्राइविंग कारें, ओशन फार्मिंग और कार्बन कैप्चर जैसी तकनीकें कार्बन रिलीज को उल्टी दिशा में मोड़ सकती हैं।
अभी तक हम उन तकनीकों पर बात कर चुके हैं जो कार्बन रिलीज को कम करने में मदद कर सकती हैं। समय समय पर कंपनियां और NGO भी नए आइडियाज लेकर आते रहते हैं। ऐसी ही तीन तकनीकों पर बात करते हैं। एक है सेल्फ ड्राइविंग कारें। ये भले ही इको फ्रेंडली ना भी लगें पर ज्यादातर कंपनियां इनको इस तरह से डिजाइन कर रही हैं कि इनसे कार्बन रिलीज कम हो। इससे फ्यूल की खपत कम होगी और कार्बन रिलीज घटेगा। इनके साथ ई मोटर, राइड शेयरिंग और ट्रैफिक राउटिंग को जोड़ दिया जाए तो और भी फायदा हो सकता है। दूसरा तरीका यानि समुद्रों को बचाना भी बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। हवा में जितनी कार्बन डाई ऑक्साइड रिलीज होती है उसमें से आधी से ज्यादा तो समुद्रों की तली में एब्जार्ब हो जाती है। हीट का भी लगभग 90% यहीं जमा हो जाता है। पर अब समुद्रों में भी इतना कचरा फैल गया है कि वो किसी उजाड़ रेगिस्तान की तरह बनते जा रहे हैं जहां ना तो समुद्री जीव बचे हैं ना पौधे।
पर समुद्रों को बचाने का तरीका भी है। यहां kelp और phytoplankton जैसे miniature plant organisms काम आते हैं। ये दूसरे पौधों, जीवों और इंसानों के लिए भोजन, फर्टिलाइजर और बायोफ्यूल का काम करते हैं। इनको समुद्रों में उगाने की तकनीक को marine permaculture कहा जाता है। इसकी मदद से algae, मछलियां, सील और शार्क का पूरा इकोसिस्टम बनाया जा सकता है। इसके अलावा तीसरे तरीके, डायरेक्ट एयर कैप्चर यानि DAC से भी मदद मिल सकती है। ये वही सिस्टम है जिसे फोटोसिंथेसिस की मदद से पेड़ पौधे सदियों से चला रहे हैं। ये हवा से कार्बन डाई ऑक्साइड लेकर इसे फ्यूल में बदल देते हैं। यहां बड़ा चैलेंज ये है कि हवा में कार्बन बस 0.04% ही है इस वजह से ये प्रोसेस लंबी और खर्चीली हो जाती है। कम से कम पेड़ पौधों वाला तरीका अपनाएं तो महंगी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आने वाले कल में DAC तकनीक को ज्यादा efficient बना दिया जाता है तो ये तरीका बहुत कारगर साबित हो सकता है। इस किताब में बताए गए उपाय उनके लिए एक उम्मीद जगा सकते हैं जो ये मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे इंसानों का हाथ है। आखिर वैज्ञानिकों ने इस दौर को Anthropocene नाम दिया है यानि जहां इंसान, एनवायरमेंट पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन नई तकनीकों की मदद से और अच्छी पॉलिसीज बनाकर हम ग्लोबल वार्मिंग के असर को रोक या बदल भी सकते हैं। क्लाइमेट चेंज भले ही इंसानों के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर नजर आ रहा हो पर इसकी वजह से हमें ये साबित करने का मौका भी मिला है कि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं।
कुल मिलाकर
अगर लोग, समाज, सरकारें और कॉर्पोरेट सेक्टर एक जुट होकर काम करें तो तो अब भी ग्लोबल वार्मिंग का असर खत्म किया जा सकता है। हमारे पास ऐसे तरीके और तकनीक मौजूद हैं जो कार्बन रिलीज कम करने और जमीन तक कार्बन वापस ले जाने में मदद करें। इसमें renewable energy को बढ़ावा देना, खेती के तरीके बदलना, जंगलों को फिर से बसाना, चीजों को रीसाइकल करना, लोगों में एनवायरमेंट को लेकर जागरुकता फैलाना, ई गाड़ियों और ओशन फार्मिंग पर ध्यान देना जैसे तरीके शामिल हैं। अगर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाएं और इन पर सब्सिडी भी मिलने लगे तो ये तरीके धरती को बचा सकते हैं।
क्या करें?
जो भी बन पाए वो करें।
परेशानी की बात ये है कि जो लोग समाज के ऊंचे और ताकतवर पदों पर बैठे हैं जैसे पॉलिसी मेकर और कॉर्पोरेट और जिनका क्लाइमेट चेंज में ज्यादा बड़ा हाथ है वही अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं। लोग सोचते हैं जब दूसरे को परवाह नहीं तो हमारे अकेले के कुछ करने ना करने से क्या होगा? लेकिन बूंद बूंद से सागर भरता है। आप कम से कम अपना कदम तो बढ़ाइए।
येबुक एप पर आप सुन रहे थे Drawdown By Paul Hawken (ed.)
ये समरी आप को कैसी लगी हमें yebook.in@gmail.com पर ईमेल करके ज़रूर बताइये.
आप और कौनसी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं. हम आप की बताई गई समरी एड करने की पूरी कोशिश करेंगे.
अगर आप का कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें ईमेल करके ज़रूर बताएं.
और गूगल प्ले स्टोर पर ५ स्टार रेटिंग दे कर अपना प्यार बनाएं रखें.
Keep reading, keep learning, keep growing.