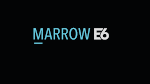Jackie Stavros and Cheri Torres
बातचीत का सलीका सिखाती किताब
दो लफ्जों में
एक पुरानी कहावत है बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पांव। इसका मतलब ये है कि अगर बातचीत का सलीका अच्छा हो तो आपको उसका ईनाम भी मिल सकता है और अगर बुरा हो तो सजा भी। बोलने को स्किल इसीलिए तो कहा जाता है। इसके महत्व का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये स्किल सीखने के लिए लोग पैसे और अपना कीमती समय तक देने को तैयार रहते हैं। साल 2018 मे आई ये किताब बताती है कि conversation की क्या ताकत होती है और हम किस तरह एक अच्छी बातचीत की मदद से अपने काम, रिश्तों और समाज में अच्छी जगह बना सकते हैं। असल जिंदगी और साइंटिफिक बातों को सामने रखकर ये किताब आपको राह दिखाती है कि किस तरह हम अपनी बातचीत का तरीका बेहतर बना सकते हैं। सही जवाब पाने के लिए जरूरी है कि आप सही सवाल करें ताकि बातचीत भी सही दिशा में जाए।
ये किताब किनको पढ़नी चाहिए?
• जो लोग किसी टीम को लीड करते हैं
• पैरेंट्स और टीचर जो बच्चों को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं
• हर वो इंसान जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहता है
इस किताब को पढ़कर आप जानेंगेये किताब किनको पढ़नी चाहिए?
• जो लोग किसी टीम को लीड करते हैं
• पैरेंट्स और टीचर जो बच्चों को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं
• हर वो इंसान जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहता है
इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे
• किसी बातचीत में छिपी ताकत
• किसी मुश्किल सिचुएशन को कैसे बदलें
• कुछ टीचर दूसरों से बेहतर क्यों होते हैं
लेखक के बारे में
जैकी स्टावरोस, लॉरेंस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनको लीडरशिप, organizational development और मैनेजमेंट में तीस साल से ज्यादा का अनुभव है। co author के तौर पर उनकी लिखी बहुत सी किताबों में Learning to SOAR का नाम खास तौर पर लिया जा सकता है। चेरि टॉरेस ने कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी ऊंची पोस्ट्स पर काम करते हुए दुनियाभर के बड़े कॉर्पोरेट्स को प्रोडक्टिविटी, कम्युनिकेशन और टीम वर्क को बेहतर बनाने में मदद की है। उनके लिखे आर्टिकल्स टॉप के अखबारों, वेबसाइट और मैग्जीन में छपते हैं। इनमें Careers in Government, Forbes और Training Magazine जैसे बड़े नाम शामिल हैं।बातचीत में पूरी तरह मगन हो जाइए।
मेलजोल और बातचीत तो इंसानी स्वभाव का हिस्सा हैं। लेकिन आपको अपने आसपास ही ऐसे कितने लोग नजर आ जाते होंगे जिनमें कुछ की बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं पर कुछ से आप दूर ही रहना चाहते हैं। असल में बातचीत के दौरान हम कैसे शब्द चुन रहे हैं और हमारा लहजा कैसा है ये काफी मायने रखता है। अगर कन्वर्सेशन पॉजिटिव रहे तो फायदेमंद साबित होता है और अच्छे रिश्ते की तरफ कदम बढ़ते हैं फिर चाहे ऑफिस हो, समाज हो या घर के रिश्ते। जबकि नेगेटिव कन्वर्सेशन तरक्की भी रोकता है और रिश्ते भी बिगाड़ता है। ये हमारे दिलो दिमाग के लिए भी नुकसानदायक साबित होता है। लेकिन अपने कन्वर्सेशन को सही और बेहतर बनाने का एक बहुत आसान रास्ता है कि आप बातचीत के दौरान सही सवाल पूछें। इसे Appreciative Inquiry कहा जाता है। इसका तरीका बहुत आसान है और इसे साइंस भी सपोर्ट करता है। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि सामने वाले तक आपकी बात सही तरह पहुंचे और उसे भी ये एहसास हो कि आप उसकी बात सही तरह सुन रहे हैं यानि उसकी वेल्यू की जा रही है। ये किताब आपको इसका तरीका समझाती है। इसमें 5 ऐसे रूल्स हैं जो Appreciative Inquiry में आपकी मदद करते हैं।
अलीशा, इंग्लैंड के एक मेडिकल सेंटर में काम करती है जहां हर दम भीड़ रहती है। किसी यूनिट से एक नेगेटिव फीडबैक आया है। मैनेजमेंट में हाल ही में बदलाव हुए हैं और काम का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से स्टाफ भी परेशान है। अलीशा, नर्सों से हेड के तौर पर बात करने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या सही कन्वर्सेशन इस तस्वीर को बदलकर सब कुछ ठीक कर सकता है? जवाब है "हां।" लेकिन इसके पहले ये देखते हैं कि अगर अलीशा सही कन्वर्सेशन न सीखती तो उसका क्या कहना होता। "रिपोर्ट में कौन सी नई बात है? हर बार ऐसी ही रिपोर्ट तो आती है। आप तो अपना रवैया बदलते ही नहीं और हर बार मरीजों की शिकायतों का ढेर लग जाता है।" इस तरह की बातचीत से तो कोई हल नहीं निकलता। स्टाफ भी और चिढ़ता कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है।
इसे depreciative कन्वर्सेशन कहा जाता है। इनसे हालात सुधरने की जगह बिगड़ते ही हैं। इसमें अलीशा का पूरा ध्यान परेशानी पर रहता न कि उसकी जड़ पर। उसे Appreciative Inquiry का इस्तेमाल करना चाहिए। उसे साथी नर्सों से पूछना चाहिए कि इस यूनिट में अच्छी बातें क्या हैं और मरीज किन बातों पर अच्छा या खुश महसूस करते हैं। इस तरह शुरुआत हो तो साथ की नर्सें खुलकर अपनी हर बात कह सकती हैं और ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे मरीजों की देखभाल भी सही तरह हो और नर्सों पर भी बोझ न बढ़े। अलीशा की बातचीत कितनी अच्छी रही ये इससे साबित हो जाता है जब बाहर निकलते हुए एक नर्स ये कहती है कि आपसे ये मीटिंग करके अच्छा लगा। हमें यकीन है कि हमारी परेशानियों का हल निकल आएगा। हर मीटिंग या बातचीत इतनी अच्छी तरह खत्म हो ये भी जरूरी नहीं है पर किसी भी बातचीत को सही ढंग से शुरू करने की अप्रोच यही होनी चाहिए। आप बात शुरू करने के पहले थोड़ी तैयारी भी कर सकते हैं।
जैसे एक आइसबर्ग पानी के ऊपर थोड़ा ही नजर आता है पर उसका एक बड़ा हिस्सा पानी के अंदर भी होता है। ऊपर से नजर आने वाले हिस्से को बातचीत ही समझ लीजिए जबकि नजर न आने वाला हिस्सा हमारी अपनी सोच, समझ, तनाव, सामने वाले से हमारा रिश्ता, उम्मीदें और तो और कल हमारी नींद कैसी थी इससे भी बदल जाता है। और जिस तरह आइसबर्ग से टकराने पर टाइटैनिक का हाल हुआ था वही नतीजा आपके रिश्तों का भी होगा क्योंकि तब भी नीचे छिपी बर्फ को नजरअंदाज कर दिया गया था। जब कभी किसी बातचीत में ऐसे छिपे हुए फैक्टर्स का असर रहता है तो ये depreciative conversation की तरफ चली जाती है। ऐसे में इसे appreciative conversation में बदलने के लिए इन छिपी हुई बातों को सामने लाने का रास्ता ढूंढना होगा। इसका आसान तरीका भी है जिसके तीन स्टेप्स हैं - pause, breathe, और get curious.
अगली बार जब कभी आपको ये लगे कि आप depreciative conversation की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एक पॉज लीजिए। इससे बात और ज्यादा बिगड़ने से बच जाती है। अब गहरी सांस लीजिए। इस तरह सांस लेने पर parasympathetic nervous system एक्टिवेट होकर तनाव को कम कर देता है। आप जितनी गहरी सांस लेंगे उतना अच्छा असर होगा। गहरी सांस लीजिए कुछ पल रुकिए और फिर धीरे-धीरे सांस छोड़िए। कुछ देर ऐसा करते रहिए। अब नंबर आता है curious होने का। दिमाग में जो चल रहा है उस पर सवाल पूछिए। अपना दायरा बड़ा कीजिए। खुद से पूछिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? ऐसा क्या है जो आप मिस कर रहे हैं? आपको क्या महसूस हो रहा है? ये छोटा सा कदम आपको उन अनदेखे फैक्टर्स की गिरफ्त में आकर गलत शब्द कहने से रोक देगा और बातचीत की कमान आपके हाथों में आ जाएगी। आगे हम इस पर और डीटेल में बात करेंगे।
Appreciative Inquiry की मदद लीजिए।
जेरी, बच्चों से जुड़े एक एनजीओ में काम करते हैं। उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। उनको 6 महीने के अंदर साउथ वियतनाम के बच्चों में फैली malnutrition की परेशानी को दूर करना है। उनको पता है कि अगर रूटीन वाले तरीके से काम किया जाए तो इतने कम समय में साफ पानी या खानपान जैसी बुनियादी बातों से हल नहीं निकलेगा। उनको लीक से हटकर सोचना होगा। वो खुद से generative सवाल करते हैं कि क्या ऐसे भी परिवार हैं जहां सेहतमंद बच्चे हैं? उनकी परवरिश किस तरह होती है? इस तरह के सवालों को generative questions कहा जाता है जहां what if, how would जैसे शब्दों से बात शुरू की जाए। इस तरह के सवाल curiosity को और बढ़ाते हुए नए सवालों को जन्म देते हैं। Appreciative Inquiry के लिए ऐसे सवाल बहुत काम आते हैं। ऐसे सवाल, छिपी हुई परेशानियों को सामने लाकर बातचीत में value add करने का काम करते हैं। सामने वाले या सिचुएशन के बारे में आपकी समझ बढ़ती है और हल समझ में आने लगते हैं।
इस तरह के सवाल करने से जेरी को भी बहुत मदद मिली। उनके सवाल का जवाब था हां, यहां सेहतमंद बच्चे भी होते हैं। अब अगला सवाल था कि इनकी परवरिश में बाकी बच्चों से क्या फर्क होता है? जेरी ने ये देखा कि ऐसे घरों में माताएं उस तरह से रूल्स फॉलो नहीं करती थीं जो बाकी घरों में होते थे। जैसे ये बच्चे दूसरे बच्चों से ज्यादा खाते थे, उनके भोजन में मीट भरपूर होता था और बीमार पड़ने पर भी उनका भोजन वैसे ही जारी रहता था। जबकि ये सारी बातें वहां के समाज के हिसाब से उल्टी थीं। लेकिन इससे उन बच्चों का न्यूट्रीशन सही बना रहा। जेरी ने generative सवाल करके इस परेशानी का बड़ा आसान हल ढूंढ निकाला था। आपको भी इस तरह के सवालों की मदद लेनी चाहिए। खुले दिल से सवाल करें और रास्ता आसान बनाते रहें। मोनिका और उसके बेटे एडन का उदाहरण ले लीजिए। एडन वीकेंड पर घूमने के लिए कार ले जाना चाहता था जबकि उसकी उम्र और ड्राइविंग के कम अनुभव को देखते हुए मोनिका इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि वो बिना किसी बड़े को साथ लिए गाड़ी लेकर निकले। कुछ देर तक बहस करते रहने के बाद मोनिका ने पूछा - आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है जहां तुम कार भी ले जाओ और मुझे तुम्हारी चिंता भी न हो।
इस सवाल ने जैसे एक नया रास्ता खोल दिया। अब दोनों एक ही दिशा में सोचने लगे। आप इस बात से generative question की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। यहां सवाल तो बदला ही पर उसे पूछने का तरीका भी बदला। इसे positive framing कहा गया है। मार्क का उदाहरण भी ऐसा ही है। वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। उनकी जूनियर मेलिसा वैसे तो बहुत अच्छी है पर उसकी एक बात खराब है कि वो हर बुधवार को होने वाली वीकली मीटिंग में हमेशा देर से पहुंचती है। मार्क को हमेशा इस बात से परेशानी होती कि वो मेलिसा की ये आदत कैसे सुधारे। अब मार्क Appreciative Inquiry की राह पकड़ता है। अगर पहले वाला मार्क होता तो उसे डांटता या कहता कि "ये क्या लगा रखा है? तुमने तो मीटिंग में हमेशा लेट आने की ठान रखी है। अपना रवैया सही करो।" लेकिन ये तो depreciative और unproductive कन्वर्सेशन हो गया। अब मार्क पॉजिटिव तरीके से अपनी बात frame करता है। वो परेशानी पर नहीं उसके हल पर सोचता है। इसमें तीन स्टेप काम आते हैं जिनको flipping कहा जाता है। वो पहले परेशानी को समझता है, फिर इसके हल ढूंढने की कोशिश करता है और फिर बातचीत का सही तरीका तैयार करता है। चलिए हम इसे और अच्छी तरह समझते हैं।
परेशानी को समझना सबसे आसान काम है। मेलिसा देर से आती है और डेडलाइन मिस कर देती है। इसका उल्टा क्या हो सकता है? वो हमेशा टाइम पर आए और डेडलाइन पूरी करे। कितना अच्छा होगा ना? लेकिन इससे क्या होगा? जेरी को लगता है इससे टीम वर्क बेहतर होगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड फील करेंगे और टीम की परफार्मेंस अच्छी हो जाएगी। बस इसी को ध्यान में रखते हुए मार्क बातचीत की शुरुआत करता है। वो मेलिसा से कहता है कि जब किसी टीम के लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं तो टीम वर्क निखरकर आता है। मेलिसा भी इस बात को मानती है। इसके बाद जब मार्क उसे ये कहेगा कि मेलिसा के देर से आने की वजह से टीम का ढांचा खराब हो रहा है तो मेलिसा ज्यादा गहराई और खुले दिमाग से इस बात को समझेगी। अब मार्क का generative question होगा कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेलिसा हर बुधवार को ही लेट हो जाती है? मार्क को जवाब मिलता है कि हर बुधवार, मेलिसा को अपने बेटे को डे केयर में छोड़ने जाना पड़ता है। अगर मीटिंग आधे घंटे आगे बढ़ा दी जाए तो सारी परेशानी हल हो जाएगी। मार्क तो मैनेजर था। चीख चिल्लाकर, डांट डपटकर मेलिसा को समय पर आने का अल्टीमेटम दे सकता था। मेलिसा काम तो करती पर आधे पोटेंशियल के साथ। लेकिन थोड़ी सी समझदारी दिखाकर मार्क ने बातचीत का रुख ही मोड़ दिया और माहौल खराब होने से बचा लिया। अब मेलिसा भी पूरे मन से काम करती है और अपना 100% अटेंशन देती है। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो पॉजिटिव फ्रेमिंग की मदद से उसे संभाला जा सकता है। इसमें हम generative questions जोड़ दें तो Appreciative Inquiry का मजबूत आधार बन जाता है। इसे ध्यान में रखकर अब हम ऐसे पांच नियम देखेंगे जो आपको बातचीत के लिए गाइड करें।
किसी भी बातचीत के साथ पांच बुनियादी प्रिंसिपल होते हैं।
इसे अच्छी तरह समझने के लिए 7वीं में पढ़ने वाले जमाल और उसके दो टीचर्स का उदाहरण लेते हैं। पहली टीचर, मिस विटिट, सोशलस्टडीज पढ़ाती हैं। जमाल को ये क्लास बहुत अच्छी लगती है और वो इस क्लास पर पूरा ध्यान देता है। दूसरी टीचर हैं इंग्लिश पढ़ाने वाली मिस समर्स। जमाल को ये क्लास कुछ खास अच्छी नहीं लगती। हर क्लास में जमाल का बर्ताव तो लगभग एक सा रहता है। क्लास में मौज मस्ती भी करता है, इधर-उधर तांक झांक भी करता है, होमवर्क भी पूरा करता है। लेकिन दोनों टीचर्स के साथ उसका अनुभव बिल्कुल अलग है। मिस विटिट तो जमाल की हर मौज मस्ती या कभी कभार बड़ी शरारत को भी नजरअंदाज कर देती हैं। उनको पता है कि इन सब हरकतों से जमाल दूसरे बच्चों से अच्छी तरह घुल मिल पाता है। खिड़की से बाहर झांकने पर उसे फोकस करने में आसानी हो जाती है। जब कभी जमाल का होमवर्क या कोई आसाइनमेंट सही नहीं होता तो मिस विटिट, Appreciative Inquiry की मदद लेती हैं। वो जमाल से जनरेटिव सवाल पूछती हैं।
जबकि मिस समर्स, जमाल को रोकती टोकती हैं। कोई होमवर्क पूरा न हो तो वो उसके बारे में सवाल करती हैं। जबकि दोनों ही टीचर्स जमाल का भला चाहती हैं और उनका इरादा ये है कि जमाल अच्छी तरह पढ़ाई करे और आगे बढ़े। लेकिन दोनों के तरीके अलग हैं। इसकी वजह समझने के लिए आपको इन दोनों टीचर्स की सोच तक जाना होगा। मिस समर्स एक बहुत स्ट्रिक्ट परिवार में पली बढ़ी हैं। उनको बचपन से ये सिखाया गया कि सफल होने के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन और फोकस बनाकर अपना काम कीजिए और आगे बढ़िए। मिस विटिट की परवरिश ऐसे घर में हुई जहां ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी। अब ये दोनों टीचर्स अपनी अपनी सोच के हिसाब से जमाल को साथ पेश आती थीं।
यहां Appreciative Inquiry का पहला नियम आता है जिसे constructionist principle कहते हैं। हमारा सोचने समझने का नजरिया समाज और आसपास के माहौल के हिसाब से डेवलप होता है। ये आगे चलकर हमारी पर्सनालिटी को आकार देता है। अगर आप ये बात समझ लेते हैं तो आगे कभी भी किसी बातचीत में इसे हावी न होने दें और खुले विचार से शुरुआत करें। अगले नंबर पर आता है simultaneity principle जो ये कहता है कि जब कभी हम बातचीत के दौरान कुछ कहते हैं या कोई सवाल करते हैं तो सुनने वाले के लिए वो बहुत मायने रखता है। जमाल के बर्ताव को इस नियम से अच्छी तरह समझा जा सकता है। इस पूरे नियम का सार बस इतना है कि अपनी बात कहने के लिए सोच समझकर शब्द इस्तेमाल करें। तीसरा यानि The poetic principle कहता है कि हर इंसान, ग्रुप या सिचुएशन को समझने का नजरिया हर किसी के लिए अलग होता है। इस नियम से हम ये समझते हैं कि आखिर क्यों मिस विटिट, जमाल की मौज मस्ती को अपने साथियों से घुलने मिलने के तरीके के रूप में देखती थीं जबकि मिस समर्स को लगता था कि इससे जमाल क्लास में फोकस नहीं कर पाएगा। सबक ये है कि आप चीजों को देखने का नजरिया बदलकर सिचुएशन को संभाल सकते हैं। The anticipatory principle कहता है कि बातचीत पर हमारी सामने वाले से लगाई गई उम्मीद भी असर डालती है। मिस समर्स के हिसाब से जमाल को behavioral issues थे इसलिए उन्होंने इसे ठीक करने की सोची जबकि मिस विटिट के हिसाब से ये जमाल की खासियत या ताकत थी इसलिए वो इस ताकत पर फोकस करती थीं।
आखिरी नंबर पर आता है The positive principle जो ये कहता है कि सवाल जितना पॉजिटिव होगा जवाब या हल भी उतना पॉजिटिव होगा। मिस विटिट ने ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सवाल करके जमाल की मदद भी की और सिचुएशन को संभाल भी लिया। इससे हमें यही सबक मिलता है कि सोच समझकर सवाल किए जाने चाहिए। आगे हम Appreciative Inquiry के कुछ तरीके सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये पांच नियम किस तरह अपने काम, घर और समाज में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
Appreciative Inquiry को आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं।
बातचीत तो हमारे समाज की बुनियाद रही है। चाहे घर हो, ऑफिस या बाहरी दुनिया हम सबको बातचीत ने ही एक दूसरे से बांध रखा है। अब तक आपने ऐसे बहुत से उदाहरण देख लिए कि किस तरह Appreciative Inquiry रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करती है। आखिरी उदाहरण जैकी की बेटी एली का ही लेते हैं। एली की उम्र तब 13 साल थी। उस वक्त स्कूल की छुट्टियां थीं। लेकिन अचानक पता चला कि उसके पिता को कैंसर है। जैकी तो ज्यादातर समय पति के साथ अस्पताल में ही रहने लगीं और एली को उनके भाई के साथ कभी एक तो कभी दूसरे रिश्तेदार के घर रहना पड़ा। वो हफ्ते में बस एक बार अपने पिता को देख पाती। जाहिर है कि वो आने वाले कल को लेकर परेशान थी और अक्सर अपनी माँ से ये सवाल करती कि पापा ठीक तो हो जाएंगे? उनको कुछ हो तो नहीं जाएगा? ऐसे में कोई भी इंसान यही कहता कि हिम्मत रखो सब ठीक होगा। पर जैकी ने कहा "देखो एली एक दिन हम सबको मरना ही है। फिलहाल हमें बस इस वक्त से गुजरना है, इसे एप्रिशिएट करना है और एक दूसरे का साथ निभाना है।" एली उस वक्त को याद करते हुए कहती है कि इस बातचीत ने जिंदगी को देखने का उनका नजरिया ही बदल दिया।
एली का नाराज होना जाहिर था, "ऐसे बुरे वक्त को मैं एप्रिशिएट कैसे करूं?" जवाब देते हुए माँ ने एक आसान से generative question से बातचीत का रुख बदल दिया - "अपने पिता के साथ बिताया तुम्हारा सबसे अच्छा पल कौन सा है?" इसके जवाब में एली को बीते वक्त की हर अच्छी बात याद आने लगी और उसके चेहरे पर खुशी छा गई। एली ने बताया कि उसे अपने पिता के साथ आंगन में बैठकर ढलता हुआ सूरज देखने में बहुत मजा आता था। तब माँ ने कहा कि आज तुम वहीं बैठकर ढलता हुआ सूरज देखना। मैं अस्पताल में कमरे का पर्दा खोल दूंगी और पापा का बेड इतना ऊंचा कर दूंगी कि वो खिड़की से बाहर देख सकें। यानि आज फिर से तुम दोनों एक साथ ढलता हुआ सूरज देखोगे। एली के पिता ने एक रोज दुनिया को अलविदा कह दिया और देर सवेर सबकी जिंदगी फिर से शुरू हो गई लेकिन एली को आज भी माँ की कही बातें याद हैं और इस बातचीत से मिला हौसला उसे हर मुश्किल वक्त में मदद करता है कि किस तरह एक बुरा माहौल खुशनुमा हो गया था। इस बातचीत ने एली को सिखाया कि कैसे हँसते हुए मुश्किलों का सामना करना है। आप भी ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। Appreciative Inquiry हर तरह के कन्वर्सेशन में मदद करती है चाहे आप दूसरों से बात कर रहे हों या अपने आप से। खुद पर इस बात का गुस्सा उतारने की जगह कि आपने आज का दिन बर्बाद कर दिया आप ये सोच सकते हैं कि आने वाले कल का वक्त किस तरह सही ढंग से इस्तेमाल करना है। अपने पार्टनर से ये कहने की जगह कि रोज शाम को बैठकर टीवी देखने से आप बोर होते हैं उनसे ये कहिए कि जब आप दोनों बाहर घूमने जाते थे तो आपको कितना मजा आता था। अगर बच्चों को घर आने में देरी हो जाए तो उनको डांटने की जगह ये कहिए कि उनके देर से लौटने पर आपको चिंता हो जाती है। हमने अलीशा का उदाहरण देखा है। अपने जूनियर्स की कमियां निकालने की जगह ये देखिए कि उनको क्या करना बेहतर लगता है और वो किस तरह खुश रहकर काम कर सकते हैं। हमारी पहचान हमारी बातों से ही होती है। इसलिए जो भी बोलें सोच समझकर बोलें।
कुल मिलाकर
इस पूरी किताब से आपको ये समझ आता है कि Appreciative Inquiry बातचीत का रवैया बदल सकती है। देखिए कि आपकी बातचीत या सोच पर असर डालने वाले छिपे हुए फैक्टर्स कौन से हैं। बातचीत को सही ढंग से करने लिए generative questions पूछिए। नतीजे देखकर आप हैरान रह जाएंगे।
क्या करें
किसी दिन अपनी बातचीत पर अच्छी तरह ध्यान दीजिए। एक कागज पर दो कॉलम बनाइए। एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव लिखिए। दिन भर आपकी जो भी बातचीत रही उसे इन दो खानों में रखिए। देखिए कि कौन सी बातचीत appreciative थी और कौन सी depreciative. ये भी लिखिए कि दोनों तरह की बातचीत के दौरान आपको कैसा लगा, आपके बोलने की टोन कैसी रही। आखिर में ये देखिए कि कितने पॉजिटिव कन्वर्सेशन हुए और कितने नेगेटिव। अगर हर तीन पॉजिटिव पर एक नेगेटिव कन्वर्सेशन या इससे कम हो तो बदलाव की जरूरत है।
येबुक एप पर आप सुन रहे थे Conversations Worth Having By Jackie Stavros and Cheri Torres.
ये समरी आप को कैसी लगी हमें yebook.in@gmail.com पर ईमेल करके ज़रूर बताइये.
आप और कौनसी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं. हम आप की बताई गई समरी एड करने की पूरी कोशिश करेंगे.
अगर आप का कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें ईमेल करके ज़रूर बताएं.
और गूगल प्ले स्टोर पर ५ स्टार रेटिंग दे कर अपना प्यार बनाएं रखें.
Keep reading, keep learning, keep growing.