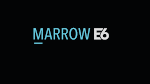Atul Gawande
बढ़ती उम्र, बीमारियों और मृत्यु को स्वीकार करने की जरूरत
दो लफ्जों में
मरने के नाम से हर कोई डरता है जबकि एक दिन सबको मरना है। इस शब्द को इतना बुरा माना जाता है कि इस पर बात करना तो दूर कोई इसका नाम भी लेना नहीं चाहता। 2014 में आई ये किताब पाठकों को जीवन के इस सबसे कठोर और अटल सत्य को समझने और स्वीकार करने में मदद करती है। इस किताब में आप मृत्यु के बारे में आधुनिक समाज के नजरिए, इससे जुड़ी संवेदनाओं और कमियों के बारे में जानेंगे। आप ये भी सीखेंगे कि इस डर को दिल से कैसे निकालना है ताकि आप जीवन को खुलकर और निश्चिंत होकर जी सकें।
यह किताब किनको पढ़नी चाहिए
- हर ऐसा व्यक्ति जो बुजुर्गों और मौत की दहलीज पर खड़े लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचता है
- जिनके घर में बुजुर्ग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं
- जो लोग अपने जीवन को सुधारकर सम्मान के साथ इस इस दुनिया से विदा होना चाहते हैं
लेखक के बारे में
अतुल, हावर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में डॉक्टर, लेखक, रिसर्चर और प्रोफेसर हैं। उन्होंने कॉम्प्लीकेशंस और द चेकलिस्ट मेनिफेस्टो नाम की दो और किताबें लिखी हैं।
बढ़ती उम्र के साथ दवाओं और लोगों पर निर्भरता बढ़ती जाती है।
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था इस दुनिया में दो ही चीजें हैं जो निश्चित हैं। एक है टैक्स और दूसरी मृत्यु। लाख कोशिश कर लें न तो आप मरने से बच सकते हैं और न टैक्स देने से। टैक्स देना थोड़ा बुरा तो लगता है पर हमने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया है। यानि टैक्स देना है तो देना है बस। लेकिन क्या हम मृत्यु को भी इसी तरह स्वीकार कर पाए हैं? जबकि टैक्स तो मृत्यु के मुकाबले बहुत बाद में आया कांसेप्ट है। मेडिकल साइंस में रोज हो रही तरक्की हमें जीने के लिए ज्यादा वक्त देती जा रही है। लेकिन मृत्यु की दिशा में हमारा सफर भी उतना ही लंबा होता जाता है। पहले लोग कम जीते थे तो शायद जिंदगी की बहुत सी परेशानियों से बच भी जाते थे। अब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ लाइफ तो आ गई है पर क्वालिटी उतनी नहीं रही। व्यक्तिगत रूप से और एक सभ्य समाज के तौर पर भी हमें मृत्यु नाम के इस कड़वे सच का सामना करना होगा। हमें मृत्यु को एक असहनीय और अशुभ शब्द के टैग से बाहर निकालकर दूसरे किसी भी शब्द की तरह आम और सामान्य बनाना होगा। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि जीवन के अंतिम वक्त तक डिग्निटी के साथ जीना क्या मायने रखता है? केयर होम्स में घर जैसा माहौल होना क्यों जरूरी है? और किस तरह मृत्यु के बारे में बात करके उसे स्वीकार करना आसान बनाया जा सकता है?
तो चलिए शुरू करते हैं!
बढ़ती उम्र के साथ दवाओं और लोगों पर निर्भरता बढ़ती जाती है।
बीमारी या मृत्यु के बारे में सोचकर किसे अच्छा लगता है? लेकिन एक दिन सबको इन रास्तों का अनुभव करना ही है। चाहे हम खुद इस पर चलें या अपने चाहने वालों को इस पर चलता देखें। जब इसे टाला ही नहीं जा सकता तो क्यों न समझदारी दिखाते हुए इसे स्वीकार कर लिया जाए? ढलती उम्र के साथ ही हमारा शरीर भी धीरे-धीरे अपनी ताकत खोने लगता है। हमारी हड्डियां, मांसपेशियां और दांत कमजोर होने लगते हैं। हमारी ब्लड वैसल्स और जोड़ स्टिफ हो जाते हैं। इस वजह से ब्लड फ्लो बनाए रखने के लिए हृदय को ज्यादा काम यानि पंप करना पड़ता है। ये एक बड़ी वजह है कि कई बुजुर्ग लोग हाई बीपी से पीड़ित होते हैं। दिमाग का आकार सिकुड़ने की वजह से दिमाग भी कमजोर होने लगता है। इससे डिमेंशिया और कई तरह की न्यूरोलॉजिकल बीमारियां घेर लेती हैं। जैसे-जैसे शरीर की एफिशिएंसी कम होने लगती है चोट और बीमारियों के चांस बढ़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से बुजुर्ग लोगों के गिरने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अगर अमेरिका की ही बात करें तो यहां हर साल लगभग 350,000 लोग इस वजह से हिप जाइंट तुड़वा बैठते हैं। उम्र बढ़ने की वजह से अपने रोजमर्रा के काम करने की ताकत भी कम होने लगती है। जैसे कि घरेलू चीजें खरीदने से लेकर वॉशरूम जाने जैसे हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। यानि अपने आखिरी साल बिस्तर पर या अस्पतालों में बिताने की नौबत आ जाती है। सब जानते हैं कि एक उम्र के बाद हाथ-पैर साथ नहीं देते। इसलिए खुद को इस दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार करना बहुत जरूरी होता है। इस तरह हम अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर आई तकलीफ का एहसास थोड़ा कम कर सकते हैं।
अस्पतालों में बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है।
मेडिकल फील्ड में हो रही तरक्की की वजह से औसत उम्र बढ़ गई है। पहले पचास साल की उम्र भी बहुत मानी जाती थी। क्योंकि इस उम्र में हुई कोई बीमारी अक्सर जानलेवा साबित होती थी। लेकिन अब बहुत सी ऐसी दवाएं और इलाज हैं जिनसे लंबे समय तक शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। यानि मृत्यु को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस वजह से अमेरिका में 65 साल की उम्र पार करने वाले लोगों की संख्या पिछले 200 सालों में 2 से बढ़कर 14 प्रतिशत पर आ गई है। जर्मनी, इटली और जापान में कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत बुजुर्ग लोग हैं। इन आंकड़ों से ये भी समझ आता है कि मृत्यु की दर और वजहों में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। मानव विकास के इतिहास में यही देखा गया है कि कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे या आसपास ही रहती थीं। जैसे-जैसे माता-पिता बुजुर्ग और शारीरिक रूप से कमजोर होने लगते बच्चे उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ले लेते। यही सिलसिला चलता रहता। इस वजह से बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में घर पर ही रहते थे। उनके पास पारिवारिक माहौल होता था। प्यार और सपोर्ट होता था। उनकी आखिरी सांस सुकून से भरी होती थी। जबकि ऐसे लोग जिनके पास परिवार का सहारा नहीं होता था वे अक्सर अपने अंतिम दिनों में अकेलेपन, गंदगी और मायूसी जैसी परेशानियों का शिकार बन जाते थे। आज की तारीख में बुजुर्गों की सेवा और देखभाल के लिए परिवार की जगह अस्पताल, डॉक्टर और नर्सों ने ले ली है। ये ध्यान देने वाली बात है कि साल 1945 में अमेरिका में ज्यादातर मौतें घर पर हुईं। 1980 का दशक आते-आते यह संख्या काफी कम होते हुए 17 प्रतिशत पर सिमट गई थी। आज के दौर में अधिकांश मौतें या तो अस्पतालों या केयर होम्स में होती हैं। ये बदलाव कैसे हुआ? इसकी एक वजह है परिवारों में बढ़ती दूरियां। बच्चे वयस्क हो जाने पर अक्सर अपने माता-पिता से दूर रहते हैं। वे उनको वक्त देने या उनकी देखभाल के लिए भी तैयार नहीं हैं। राहत की बात ये है कि आज के ज्यादातर अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में हर तरह की मेडिकल केयर मिलने लगी है। इस तरह उन लोगों को भी पूरी तरह से सुरक्षित और साफ-सुथरा माहौल मिल जाता है जिनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। यहां अच्छे तरीके से देखभाल तो हो जाती है पर परिवार का प्यार नहीं मिल पाता जिसकी हर इंसान को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
बुजुर्ग व्यक्ति ये चाहते हैं कि अपने कुछ काम खुद ही करें न कि हर चीज में दूसरों का सहारा लें।
जब आप छोटे होते हैं तो आपके पास बहुत आजादी होती है। आप अकेले रह सकते हैं। जो मन आए वो हरकतें और उछल कूद कर सकते हैं। ऐसा करते हुए किसी तरह की घबराहट नहीं होती क्योंकि आपका शरीर आपका पूरी तरह से साथ देता है। हर मौसम अच्छा लगता है। सर्दी में आइस्क्रीम और बरसातों में भीगना मजा देता है। हां बड़ों का डर और डिसिप्लिन होता है पर बच्चे इसकी परवाह ही कितनी करते हैं? क्योंकि आजादी और मनमर्जी से रहना हर इंसान की पहली ख्वाहिश होती है। ये हमारी बेसिक जरूरत भी है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी में एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब आजादी शब्द का मतलब बदल जाता है। जब आप बूढ़े हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं तो आपका शरीर और मन पहले की तरह मजबूत नहीं रह जाता। सर्दी में दूसरों से ज्यादा ठंड लगने लगती है। बरसात तरह-तरह के इन्फेक्शन ले आती है। दौड़-भाग करना तो सपने में भी मुश्किल लगता है। कुल मिलाकर आपकी वर्तमान अवस्था जिंदगी में तरह-तरह की पाबंदियां लगाकर अब तक मिली आजादी छीन लेती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी लगाम दूसरों के हाथ में देने के लिए खुद को एकदम से तैयार कर लें। आखिर इतने साल आप अपनी मर्जी से जीते आए हैं। तो एकदम से इस बदलाव को स्वीकार कैसे किया जा सकता है। इसलिए हम बुढ़ापे में भी पहले की तरह आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। हम यह महसूस करना चाहते हैं कि आज भी हमारे जीवन का कोई उद्देश्य और मूल्य है। हम ये भी समझते हैं कि बुढ़ापे में हम वो सब कुछ नहीं कर सकते जो पहले करते आए थे फिर भी हम थोड़ी आजादी बनाए रखना चाहते हैं। मान लीजिए आपको कुकिंग का शौक था। उम्र ढलने के साथ अब किराने के सामान खरीदना मुश्किल बन जाता है। ऐसे में बजाए कुकिंग पूरी तरह से छोड़ने के आप शॉपिंग में मदद लेने की बात सोचते हैं।
जैसे-जैसे हम यह महसूस करते लगते हैं कि हम अपने जीवन के आखिरी पायदान की तरफ बढ़ रहे हैं जिंदगी की तरफ हमारा नजरिया बदल जाता है। हम बजाए नई चीजों और चाहतों के पीछे भागने के अपने रोजमर्रा की बातों में ही खुशियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे खाना बनाना, गार्डनिंग और धार्मिक गतिविधियां। परिवार और दोस्तों के साथ हमारा लगाव बढ़ने लगता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक लॉरा कार्स्टन ने एक स्टडी की। इसमें भाग ले रहे लोगों को ये बताना था कि वो किनके साथ अपना वक्त बिताना ज्यादा पसंद करेंगे। ऑप्शन के तौर पर उनकी माँ, पसंदीदा लेखक, जान पहचान के लोग और अजनबी लोग दिए गए। जो लोग युवा थे उन्होंने नए और अजनबी लोगों के साथ समय बिताने के लिए उत्सुकता दिखाई। जबकि बुजुर्ग और एचआईवी पॉजिटिव लोगों ने अपने परिवार के लोगों और दोस्तों के साथ समय बिताने का विकल्प चुना। उम्र के साथ आप पहले से ज्यादा शांत और स्थिर होने लगते हैं। फिर भी ज्यादातर लोग बुढ़ापे से डरते हैं। दरअसल इस उम्र में सबसे ज्यादा जरूरी कुछ होता है तो वो है अपनेपन का एहसास। लेकिन केयर होम्स इस जरूरत को पूरा करने में असफल रह जाते हैं। अगले लेसन्स में हम इस पर और बात करेंगे।
मेडिकल केयर सेंटर में बुजुर्गों को वो आजादी और भावनात्मक सपोर्ट नहीं मिलता जिसके लिए वो तरसते हैं।
जब कोई वृद्धाश्रम के बारे में सोचता है तो वो बोरियत और अकेलेपन के एहसास से भर उठता है। ये सोच हकीकत के बहुत नजदीक है। हमारे समाज में बुजुर्गों के लिए बोरियत और अकेलापन बड़ा सामान्य मान लिया गया है। नर्सिंग होम और केयर यूनिट अक्सर एक फिक्स रूटीन और नियम के अनुसार काम करते हैं। जो लोग कभी अपने मन मुताबिक जीने और रहने के आदी थे यहां आकर खुद को एकदम से कैद में महसूस करने लग जाते हैं। उनके पास पर्सनल स्पेस या लाइफ जैसा कुछ नहीं रहता। क्योंकि केयर सेंटर में उनकी निगरानी भी जरूरी होती है। देखभाल करने वाली नर्सों और अटेंडेंट्स का रवैया बिल्कुल प्रोफेशनल और मेकेनिकल होता है। थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मरीज या बुजुर्ग अपने कपड़े खुद पहन सकते हैं। पर नर्स के लिए उनको कपड़े पहना देना ज्यादा टाइम सेविंग हो जाता है। लेकिन इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। नर्स तो अपना काम करके चली जाती है पर ये लोग इस बात से खुद को बेकार, कमजोर और अक्षम महसूस करने लगते हैं कि अब उनको कपड़े बदलने तक के लिए दूसरों की जरूरत पड़ने लगी है। वृद्धाश्रम या अस्पताल देखभाल और सुरक्षा तो अच्छी देते हैं। पर वहां रह रहे बुजुर्ग लोग घर जैसा महसूस नहीं कर पाते। उनके शरीर की देखभाल हो जाती है पर मन की तकलीफ बनी रहती है। हालांकि इस केयर के महत्व को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वे बुजुर्गो और मरीजों को नहलाते हैं, उनको साफ-सुथरा रखते हैं। समय पर खाना खिलाते हैं। इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि हर कोई समय पर दवा लेता रहे। लेकिन इतना काफी नहीं है। जीवन के हर मोड़ की तरह बुढ़ापे में भी प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है। बुजुर्ग चाहते हैं कि लोग उनकी जरूरतों और बातों को समझें। वृद्धाश्रमों और मेडिकल सेंटर्स में अक्सर स्टाफ की कमी रहती है। नर्सिंग होम्स में वृद्धों की देखभाल के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमेशा से कम रहे हैं। जाहिर है जितने लोग वहां काम कर रहे हैं उन पर काम का दबाव ज्यादा है। इसलिए वो अपने मरीजों या बुजुर्गों को थोड़ा ज्यादा समय देकर स्पेशल फील नहीं करा पाते। इस कमी का एकमात्र विकल्प परिवार है। हालांकि बुजुर्गों या बीमारों की देखभाल और उनकी जरूरतों को समझना और पूरा करना काफी मुश्किल है। इसलिए कई बार परिवारों की तरफ से भी कमी रह जाती है।
बीमारी और तरह-तरह की तकलीफों के होते हुए भी हर कोई और जीने की चाहत रखता है। हम अक्सर उस तरीके या इलाज की तलाश में रहते हैं जो हमें सबसे ज्यादा दिनों तक जीने में मदद करता है। भले ही ये "ज्यादा" दिन हमारी तकलीफ को कम न कर पाएं। अमेरिका में हेल्थ केयर का पच्चीस प्रतिशत उन लोगों के लिए खर्च होता है जो अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रहे होते हैं। जबकि बाकी मरीजों की तुलना में उनकी संख्या कुल पांच प्रतिशत ही होती है।
इनमें से कुछ इलाज निश्चित तौर पर फायदा करते हैं पर ज्यादातर बस डूबती हुई सांसों को बनाए रखने जितनी मदद कर पाते हैं। इन तरीकों से मौत की आहट को धीमा जरूर किया जा सकता है पर ये जिंदगी मरीज की तकलीफ बढ़ाती ही है। ऐसे केसेज में मरीज और डॉक्टर एक झूठी कोशिश कर रहे होते हैं। मरीज के घर वाले ये समझते हैं कि अब बात डॉक्टर के हाथ से निकल चुकी है। फिर भी वे ऐसे चमत्कार की उम्मीद लगाए रहते हैं जिसका होना लगभग नामुमकिन होता है। डॉक्टर अक्सर लोगों को सही कंडीशन समझाने में बेबस हो जाते हैं। वे मरीजों और उनके परिवार की उम्मीदों को टूटने से बचाने के लिए झूठी तसल्ली देने लगते हैं। 40 प्रतिशत से ज्यादा कैंसर विशेषज्ञ ये बात मानते हैं कि अपने करियर में किसी न किसी वक्त उन्होंने ऐसे ट्रीटमेंट किए हैं जिसके नतीजे शून्य रहने के बारे में उनको पहले से पता था। इस वजह से लाइलाज या गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग अक्सर ऐसे इलाज के लिए तैयार हो जाते हैं जो काफी रिस्की होता है। इनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। जिंदगी के कुछ और वक्त मिल जाने के बदले ये एक बहुत बड़ी कीमत साबित होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी में यकीन रखते हैं। किसी के इस दुनिया से चले जाने पर हमेशा ये कहा जाता है कि वो तो बहुत कम उम्र में चला गया या फिर उसकी तो उम्र हो गई थी। पर कोई ये नहीं कहता कि उसने एक अच्छी या भरपूर जिंदगी जी। जिंदगी में कितने दिन रह गए हैं उसकी चिंता करने से अच्छा है हर पल को जिंदगी की तरह जी लिया जाए।
अमेरिकन कोपिंग विद कैंसर प्रोजेक्ट की तरफ से एक स्टडी हुई। इससे पता चला कि गंभीर रूप से बीमार कैंसर के जिन मरीजों ने इलाज की जगह घर पर अपनों के साथ वक्त बिताना पसंद किया उनका आखिरी वक्त इंटेंसिव केयर में रह रहे मरीजों की तुलना में बहुत आराम से कट गया। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां और वृद्धावस्था में होने वाली दूसरी बीमारियां डॉक्टरों, मरीजों और उनके रिश्तेदारों के सामने ऐसे सवाल रख देती हैं जिनका सही जवाब आज तक ढूंढा नहीं जा सका है। कब तक इलाज करना है? कब इसे बंद करना है? जीवन के बचे हुए दिन सुकून से कैसे काटें? इनका एक जवाब दे पाना सच में मुश्किल है।
एजिंग और डेथ जैसे विषयों पर ज्यादा बात की जानी चाहिए ताकि लोग अपना बचा हुआ वक्त सकारात्मक तरीके से बिता सकें। मृत्यु के दरवाजे पर खड़े लोगों के मन को शांत करने का तरीका तो एडवांस मेडिसिन भी नहीं ढूंढ पाई है। ऐसा क्या किया जाए जिससे वो एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकें? वे खुद को बोझ न समझने लगें इसके लिए बहुत जरूरी है कि वे किसी न किसी रूप में आत्मनिर्भर बने रहें। इसके लिए उनको सलाह और मदद दी जा सकती है। असिस्टेड लिविंग ऐसा ही एक मॉडल है। इसमें मरीजों को वैसी ही सेवा दी जाती है जो आम नर्सिंग होम या केयर सेंटर में मिल रही है। लेकिन इसका तरीका बहुत अलग है। यहां मदद ले रहे लोगों को कुछ जगह दी जाती है। इस जगह में वे अपना "घर" बना सकते हैं। वे इस बात का फैसला खुद कर सकते हैं कि उनको अपना समय कैसे बिताना है, किस तरह के काम करने हैं और किन चीजों में दूसरों की मदद लेनी है। लेखक इस तरीके के फेवर में हैं। हालांकि इसके साथ और भी विकल्प हैं जिन पर विचार किया जा सकता है।
इस बारे में न्यूयॉर्क के एक नर्सिंग होम का उदाहरण देना बहुत जरूरी है। यहां मरीजों के लिए एक बगीचा बनाकर उनको देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। पास के किंडरगार्टन से रोज बच्चों को बुलाया जाता। इसके अलावा वहां दो कुत्ते, चार बिल्लियां और 100 पक्षी भी लाए गए। दो ही सालों में सुखद नतीजे सामने आए। हर मरीज की दवाएं आधी हो गईं। मृत्यु दर सालाना 15 प्रतिशत घट गई। और ये सब हुआ कैसे? बच्चों, जानवरों और पौधों की देखभाल ने मरीजों में खुशी और उत्साह की एक नई भावना दी। उनके जीवन को एक नया मकसद मिल गया। यानि अब उनको जीने की एक वजह मिल गई। दूसरी जगहों पर भी ऐसे बदलाव किए जाने चाहिए। वे अपने साथ इसी अनुभव को लेकर विदा होते हैं जो जीवन के इस पड़ाव पर उनको मिलता है। नर्सों, डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इलाज से ज्यादा उनके इस अनुभव को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उम्र बढ़ने और इलाज के नए तरीके आने के साथ ये और भी जरूरी होता जाता है कि हम डॉक्टरों और परिवार को अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बारे में खुलकर बता सकें।
मौत की दहलीज पर खड़े लोगों को डॉक्टरों की तरफ से सही सलाह मिलनी चाहिए।
डॉक्टर और मरीज का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। वे एक दूसरे से किसी परेशानी या गंभीर परिस्थिति में ही मिलते हैं। डॉक्टर भी एक आम इंसान है। वो भी प्रोफेशनल जिम्मेदारी और इंसानी स्वभाव के डाइलेमा के बीच फंसे रहते हैं। लेकिन अपने मरीजों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने के लिए दोनों का संतुलन होना जरूरी है। न तो पूरी तरह प्रोफेशनल तरीका अपनाना चाहिए। जैसे कि मरीज को देखा, दवाई दी, पैसे लिए और काम खत्म। इसी तरह अगर मानवीय गुण जैसे दया, स्नेह ज्यादा होंगे तो डॉक्टर, मरीज के दर्द में खुद जकड़ जाएगा। उनको चाहिए कि वे बीच का रास्ता निकालें। मरीज को नर्म लहजे में उसकी बीमारी का सच बता दें। हर तरह का इलाज, उसकी लिमिटेशन और साइड इफेक्ट समझा दें। अब मरीज को फैसला लेने दें। इसके बाद उनकी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है। यानि इलाज शुरू हुआ और मरीज को उसके हाल पर छोड़ दिया। उसको समय-समय पर मोटिवेट करना भी जरूरी है।
उदाहरण के लिए अगर कोई मरीज अपनी लास्ट स्टेज पर है तो उसे पूछें कि वो बाकी का वक्त किस तरह बिताना चाहता है। हो सकता है वो किसी आउटडोर गेम खेलते हुए ये वक्त बिताना चाहे। हो सकता है उसे बाकी वक्त अपने परिवार के साथ बिताने का मन हो। जब उसकी इच्छा पता चल जाए तो इलाज के सारे विकल्प उसके सामने रख दीजिए जो उसके लिए सही हैं। जरूरी नहीं कि इस इलाज में उसे जीने के लिए और ज्यादा वक्त मिल पाए। लेकिन अगर कोई तरीका उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर सकता है तो हो सकता है मरीज वक्त की परवाह किए बगैर उसे ही अपना ले। बहुत गंभीर मामलों में डॉक्टरों को इस बात की इजाजत दी जानी चाहिए कि वो सुकून से मरीज को हमेशा के लिए सो जाने में मदद करें। ये लेखक के अपने विचार हैं। और ये मुद्दा बहुत विवादास्पद है। फिर भी डॉक्टरों को कम से कम उन लोगों के साथ इस विषय पर बात की जानी चाहिए जो अपनी बीमारी की वजह से बहुत बुरी तरह से तड़पते हैं। ज्यादातर देशों में ऐसी एक्टिविटीज बैन हैं। फिर भी मेडिकल एडवाइस उनकी कुछ मदद जरूर कर सकती है। आज की तारीख में एजिंग और डेथ परिवार के दायरे से बाहर आकर अस्पतालों और केयर सेंटर्स से भी जुड़ चुकी है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि इस फील्ड में काम कर रहे लोग अच्छी तरह मरीज और उसके परिवार की बात सुनें और समझें। इस तरह वो मरीज की ज्यादा मदद कर पाएंगे।
घरों में एजिंग, बीमारियों और मृत्यु जैसे विषयों पर खुले दिमाग से बात की जानी चाहिए ताकि कोई अधूरी इच्छाएं लेकर इस दुनिया से विदा न हो। हम बुजुर्ग अवस्था या मृत्यु जैसे विषयों पर सहज होकर बात नहीं करते हैं। इसमें कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अपनी तो क्या किसी की भी मृत्यु की कल्पना करना तकलीफदेह होता है। इसके बारे में बात तब शुरु की जाती है जब वक्त पहले ही हाथ से निकल चुका होता है। तब न तो मरीज के पास कोई इच्छा बचती है न परिवार के पास उसे पूरा करने का समय। हर किसी को सम्मान के साथ इस दुनिया से विदा होने का हक है। अगर समय रहते उनकी जरूरतों को समझकर पूरा कर दिया जाए तो उनके चले जाने के बाद इस बात की तसल्ली रहती है कि वे अपनी हर इच्छा पूरी करके गए। वरना दिल में एक कसक रह जाती है। बढ़ती उम्र और बीमारी के बारे में आने वाले विचार और सवालों पर परिवार और दोस्तों के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपने अपने आखिरी दिनों के लिए कुछ सोच रखा है तो घर पर इसकी जानकारी देनी चाहिए। आखिरी पलों में आप क्या करना चाहते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जिसे करके आपको लगेगा कि अब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही?
आपको इन सवालों जवाब अभी के अभी देना जरूरी नहीं है। लेकिन इस तरह की बातचीत से आपके आसपास के लोगों को ये समझ आ जाता है कि आपके लिए अंतिम समय में क्या किया जाना चाहिए। ये चर्चा उस वक्त आपके अपनों के बहुत काम आती है जब आप कुछ बताने की कंडीशन में नहीं रहते। इस वक्त कम से कम वो आपके लिए जो भी फैसला लेंगे आपकी दी हुई उसी जानकारी के आधार पर लेंगे। मृत्यु के आने में वक्त है। पर अगर आप आज ही अपने आखिरी दिन के बारे में सोच लेते हैं तो अपने हर डर से मुक्ति पा सकते हैं। जब आपको किसी तरह का डर नहीं रहेगा तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे और अंत तक बने रहेंगे। मृत्यु नाम की सच्चाई को स्वीकार करके आप ये तय कर सकते हैं कि जाते हुए इस दुनिया को क्या देकर जाएंगे। अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। और लोग आपको किस तरह याद रखेंगे। क्योंकि ऐसा न करने पर अंतिम वक्त में याद आता है कि हमें जो कुछ करना था वो तो किया ही नहीं।
लेखक की बेटी की पियानो टीचर ने कैंसर की लास्ट स्टेज में ऐसा ही कुछ किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर बच्चों को एक आखिरी क्लास दी। इस तरह उन्होंने अपने छात्रों के संगीत के माध्यम से खुद को हमेशा जीवित रखने का तरीका बना दिया। वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का खुलकर सामना करके हम व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक तौर पर मृत्यु को कम तकलीफदेह अनुभव बनाने में सक्षम हो सकते हैं। यहां तक कि हम इसमें भी एक उद्देश्य ढूंढ सकते हैं।
कुल मिलाकर
भले ही हम इस बारे में सोचना पसंद करें या न करें, हम सबको एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। खुशकिस्मती से हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है कि हम इस अंतिम यात्रा की तैयारी कर सकें। हमें इस बात पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि इस जीवन में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। फिर इन विचारों और जरूरतों को अपने परिवार, दोस्तों और डॉक्टरों के साथ शेयर करना चाहिए। ताकि वे इसे पाने में हमारी मदद कर सकें। इस तरह हमारा बाकी बचा जीवन खुशी और संतुष्टि से भर सकता है।
येबुक एप पर आप सुन रहे थे Being Mortal By Atul Gawande.
ये समरी आप को कैसी लगी हमें yebook.in@gmail.com पर ईमेल करके ज़रूर बताइये.
आप और कौनसी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं. हम आप की बताई गई समरी एड करने की पूरी कोशिश करेंगे.
अगर आप का कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें ईमेल करके ज़रूर बताएं.
और गूगल प्ले स्टोर पर ५ स्टार रेटिंग दे कर अपना प्यार बनाएं रखें.
Keep reading, keep learning, keep growing.