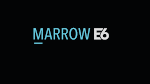David Attenborough
एक नेचर लवर की चिंता
दो लफ्जों में
कहते हैं constant is the only variable यानि बदलाव जीवन का सच है। समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा है लेकिन नेचर खुद में उतनी तेजी से बदलाव नहीं लाता है जितना इंसान अपनी हरकतों से लाता रहा है। साल 2020 में आई ये किताब धरती पर हुए उन बदलावों को आपके सामने लाकर रखती है जो जाने माने नेचर एक्सपर्ट डेविड अटेनबर्ग ने अपनी 94 सालों की जिंदगी में देखे हैं। लेकिन इन बदलावों के साथ धरती एक चेतावनी भी देती है कि अगर हमने अपने तौर तरीके ना बदले तो क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस किताब पर नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है।
ये किताब किनको पढ़नी चाहिए?
• जो लोग नेचर में रुचि रखते हैं
• जिनको ग्लोबल वार्मिंग की परवाह है
• जो लोग समय रहते अपने प्लानेट को बचाना चाहते हैं
इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे
• व्हेल्स पर बनाए गाने की वजह से कैसे उनको बचाने का कानून बना
• अगर हम अपने तौर तरीके नहीं बदलते हैं तो साल 2100 में ये दुनिया कैसी लगेगी
• पेट्रोलियम की जगह ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करना एनवायरमेंट के लिए सबसे अच्छा कदम क्यों हो सकत
है
लेखक के बारे में
डेविड पिछले 60 सालों से ज्यादा वक्त से नेचुरल हिस्ट्री पर प्रोग्राम बनाते आ रहे हैं। उन्होंने दुनियाभर की सैर की है और बहुत से अनोखे और रेयर जीवों की जानकारी ढूंढकर लाए हैं।
उम्र बढ़ने के साथ नेचर के लिए डेविड का प्यार, चिंता में बदल गया।
26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल जो आज यूक्रेन का हिस्सा है, वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका हुआ। यूरोप में इतना रेडियोएक्टिव मटेरियल फैल गया जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए एटम बम से चार गुना ज्यादा था। ये बारिश की बूंदों की तरह रिसकर धरती के अंदर भी चला गया। ये फूड चेन में भी मिल गया। अंदाजा लगाया जाता है कि इसने लाखों जानें ले लीं। चेर्नोबिल, इतिहास के सबसे बड़े इंसानी हादसों में से एक था। लेकिन आज हम इससे भी बड़े खतरे के बीच जी रहे हैं जो हमारी आंखों के सामने ही है। ये और कुछ नहीं बल्कि हमारा गलत और लापरवाह रवैया है जहां हमने बायो डायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वैसे इसमें पूरी गल्ती हमारी भी नहीं है। हमारी पहली पीढ़ी जिसने तरह-तरह की सुख सुविधाएं बनाईं उसे ये एहसास भी नहीं था कि उसने आने वाली पीढ़ी के हाथ में वरदान की शक्ल में श्राप दे दिया है। लेकिन राहत की बात ये है कि आज भी हमारे पास थोड़ा ही सही पर इतना वक्त तो बचा है कि हम हालात काबू में कर लें।
बचपन में डेविड घंटों अपने गांव और उसके आसपास साइकिल चलाते हुए ammonites ढूंढते रहते। Ammonites, घोंघे के फॉसिल को कहा जाता है। सदियों तक लाइमस्टोन में दबे रहकर फॉसिल बन चुके ये घोंघे डेविड को इतने अच्छे लगते कि इनकी वजह से डेविड ने नेचर को ही अपना करियर बना लिया। आगे उनको ये पता चला कि इन घोंघों की पूरी स्पीशीज एनवायरमेंट में अचानक हुए बदलाव की वजह से खत्म हो गई थी। हमने लगभग 175 मिलियन साल पहले डायनासोर का राज खत्म होने का किस्सा तो सुना ही है। इन लाखों सालों के दौरान जीवन दुबारा शुरू होता रहा और इंसान पनपते रहे। इंसानों में उनसे पहले रह रहे जीवों से कुछ खास फर्क था - कल्चर का। अपने कल्चर और नॉलेज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बांटने की आदत ने इंसानों को नेचर में बदलाव करके उसे अपने रहने के लिए और आसान बनाने की ताकत दी। इस ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आई। आज हम जिस हिस्से को मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं वहां आज से लगभग दस हजार साल पहले लोगों ने खेती और जानवर पालने की शुरुआत की। वहीं कुछ लोग खेती में समय देने की जगह अपनी बनाई चीजें जैसे कपड़े और घरेलू सामान की अदला बदली से काम चला लेते थे। ये सिविलाइजेशन की शुरुआत थी। लेकिन ऐसी किसी भी सिविलाइजेशन में एनवायरमेंट का मजबूत होना सबसे जरूरी था।
डेविड ने साल 1952 में एक अनाउंसर के तौर पर BBC में काम शुरू किया। आगे तरक्की करते हुए वो ये देखते गए कि किस तरह इंसान एनवायरमेंट को कमजोर बनाते आ रहे हैं। इंसानों के कामकाज की वजह से बायो डायवर्सिटी तो खराब हो ही रही थी पर पूरी की पूरी स्पीशीज भी खत्म होने लगी थीं। 1978 में डेविड पहाड़ी गोरिल्ला पर एक सीरीज बनाने के लिए रवांडा गए। वहां उन्होंने जो देखा उसने उनकी पूरी सोच बदल दी। वो एक किस्सा खास तौर पर याद करते हैं जब एक फीमेल गोरिल्ला झाड़ियों से अचानक निकलकर उनके सामने आ गई और उनके साथ खेलने लगी। उसके दो छोटे बच्चे भी डेविड के पैरों और जूतों के साथ शैतानी करने लगे। इन गोरिल्लाओं के लिए वो काफी मुश्किल का समय था। उनकी आबादी 300 से भी कम रह गई थी। लोग अपनी जरूरतों के लिए जंगल काटते जा रहे थे। इसके अलावा शिकारी भी गोरिल्लाओं के पीछे पड़े थे। इस घटना ने डेविड को एहसास दिलाया कि हम किस तरह धरती को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसकी भरपाई भी करनी मुश्किल है। लेकिन डेविड के लिए ये तो बस शुरुआत थी।
डेविड जैसे-जैसे दुनिया घूमते गए नेचर के लिए उनकी चिंता बढ़ती गई।
1970s के आखिरी सालों में डेविड का करियर पीक पर आ चुका था। उनकी बनाई सीरीज "लाइफ ऑन अर्थ" को दुनिया के लाखों लोग देख चुके थे। 1978 में बनी इस सीरीज में 30 से भी ज्यादा देशों के 200 से ज्यादा जानवरों को फिल्माया गया था। इस सीरीज से डेविड को नेचुरल हिस्ट्री को उस तरह से दुनिया के सामने लाने का मौका मिला जिसे उससे पहले कभी नहीं दिखाया गया था। वो नेचर में हो रहे बदलावों के गवाह भी बने। डेविड के लिए ब्लू व्हेल की स्टोरी कवर करना बहुत हैरानी वाला प्रोग्राम साबित हुआ। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। समुद्र का इको सिस्टम बनाए रखने के लिए ब्लू व्हेल बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं फिर भी बीसवीं सदी में इंसानों ने लगभग तीस लाख व्हेल्स को मार डाला। इस वजह से ब्लू व्हेल खत्म होने के कगार पर आ गई थी। लेकिन ये सिर्फ व्हेल्स की कहानी नहीं थी। अगले कुछ सालों में डेविड ने हर जगह यही होते देखा। रेन फॉरेस्ट, बायो डायवर्सिटी का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हैं। जमीन पर पाए जाने वाले जीवों में से लगभग आधे तो रेन फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। लेकिन हम अंधाधुंध तरीके से इन जंगलों को काटते जा रहे हैं। साल 1989 में जब डेविड साउथ ईस्ट एशिया गए तो उस वक्त तक दो मिलियन हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट काटकर वहां पाम ऑयल देने वाले पेड़ लगाए जा चुके थे। ये जगह कोलंबिया के बराबर है। आज की तारीख में दुनिया के आधे रेन फॉरेस्ट साफ हो चुके हैं। नॉर्थ और साउथ पोल भी इससे बच नहीं पाए हैं।
जब साल 2011 में डेविड, फ्रोजन प्लानेट नाम की सीरीज बना रहे थे तो दुनिया का तापमान उनके पैदा होने के वक्त से एक डिग्री सेंटीग्रेट ज्यादा हो चुका था। पिछले दस हजार सालों में हुआ ये सबसे बड़ा बदलाव था। अब दोनों पोल्स पर गर्मी का मौसम पहले से लंबा होने लगा है। ये आने वाले परेशानियों की तरफ बड़ा इशारा है। हमने पेट्रोलियम इस्तेमाल करके समुद्रों को भी जहरीला बना दिया है। जब हम कोयला और नेचुरल गैस जलाते हैं तो बहुत सारी कार्बन डाई ऑक्साइड हवा में रिलीज होती है। इसकी वजह से समुद्रों में एसिड का लेवल और तापमान बढ़ता है और कोरल रीफ खात्मे पर आने लगती है। जबकि समुद्र के पानी को सही रखने और बायो डायवर्सिटी बनाने रखने में इनका बड़ा हाथ होता है। डेविड के प्रोग्राम ने अपना असर डाला। उनकी टीम ने पहली बार किसी व्हेल को गाते हुए रिकॉर्ड किया था। इसने लोगों का ध्यान खींचा और व्हेल्स के लिए काम करने वाले लोगों ने इकट्ठे होकर सरकार को इस बात के लिए तैयार किया कि वो इनके शिकार पर रोक लगाए। अगर आज व्हेल्स की आबादी फिर से बढ़ रही है तो इसके लिए यही कदम जिम्मेदार है। लेकिन अगर हम कोई सख्त कदम ना उठाएं तो धरती की बर्बादी को कोई नहीं रोक पाएगा।
हमारे पास अब भी कुछ वक्त बचा है।
आज डेविड 90 साल से ज्यादा के हो चुके हैं। WWII खत्म होने पर उनकी उम्र 19 साल की थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1950s में की। ये एक ऐसा दौर था जब तरह-तरह की नई तकनीकें हमारी दुनिया में दखल देना शुरू कर रही थीं। लोग मानने लगे थे कि हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोच पा रहा था कि सब कुछ पा लेने का जुनून कितना खतरनाक साबित हो सकता है। 1950s को the Great Acceleration का दौर कहा जाता है। हर चीज पहले से बढ़ रही थी। लोगों की जिंदगी, आबादी, फसलों की पैदावार, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की गिनती और कार्बन की मात्रा भी। लेकिन नेचर के बर्दाश्त करने की भी एक सीमा है। कोई भी बायोलॉजिस्ट आपको ये बात अच्छी तरह बता सकता है कि आगे इसका क्या अंजाम होगा। जब धीरे-धीरे करके सारे रिसोर्स खत्म होने लगेंगे तो आबादी भी घटने लगेगी। अगले 90 साल Great Decline का दौर है। आज से कुछ ही सालों बाद 2030 में अमेजन के रेन फॉरेस्ट खत्म हो चुके होंगे। इनको वैसे भी इतनी तेजी से काटा गया है कि यहां बादल पकड़ने और बारिश कराने की ताकत ना के बराबर रह गई है। बायो डायवर्सिटी का खत्म हो जाना किसी तांडव से कम नहीं है। ऊपर से रेन फॉरेस्ट ना रहने पर बाढ़, सूखा और जंगल में आग लगने के खतरे बढ़ जाएंगे। पेड़ कम होने का मतलब है कार्बन का बढ़ना यानि ग्लोबल वार्मिंग।
आर्कटिक वाले इलाके में भी तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। इसकी वजह से 2030 की गर्मियां पहली बार आइस फ्री हो जाएंगी। आम तौर पर ये सफेद बर्फ सूरज की रोशनी को वापस भेज देती है और तापमान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता पर जब बर्फ ही नहीं रहेगी तो ये नेचुरल एयर कंडीशनर भी काम नहीं करेगा। इसके अगले दस सालों यानि 2040 तक आर्कटिक की
permafrost भी खत्म हो चुकी होगी। बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में जमीन की ऊपरी परत बर्फ की तरह जम जाती है। इसे permafrost कहा जाता है। इसके खत्म हो जाने से लैंड स्लाइड और बाढ़ आने लगेगी। लेकिन इन permafrost में पानी के साथ कार्बन गैस भी भरी रहती है। इस तरह करीब 1,400 गीगाटन कार्बन रिलीज होगी। ये कह लीजिए कि एक ऐसा वॉल्व खुल जाएगा जिसे हम बंद नहीं कर पाएंगे। 2050 तक समुद्रों का पानी इतना एसिडिक हो चुका होगा कि इसके 90% कोरल रीफ खत्म हो जाएंगे। मछलियां भी नहीं रहेंगी। इस वजह से फिशिंग इंडस्ट्री भी नहीं बचेगी। लेकिन समुद्र ही नहीं जमीन पर उगने वाली चीजें भी खत्म होने लगेंगी। क्योंकि मिट्टी और उसे फर्टाइल बनाने वाले micro organism दोनों ही बर्बाद हो चुके होंगे। साल 2100 आते आते हालात इतने खराब हो चुके होंगे कि दुनिया की बड़ी आबादी जिंदा रहने की कोशिश में माइग्रेट करने को मजबूर हो जाएगी। काफी शहर पानी में डूब चुके होंगे और दुनिया का एवरेज तापमान 4℃ तक बढ़ चुका होगा। यानि एक चौथाई आबादी उस तापमान में रहेगी जो आज सिर्फ सहारा में ही महसूस होता है। हममें से कोई भी ऐसी हालत में नहीं पहुंचना चाहता। तो इसे होने से रोकें कैसे?
सबसे पहले आबादी पर ध्यान देना होगा।
अभी आपने आने वाले कल की एक झलक देखी। हम ऐसा वक्त नहीं चाहते हैं जहां लोगों का जीवन इतना बदतर हो जाए। लेकिन अगर हम अभी भी उसी रास्ते पर चलते रहे तो ऐसा होकर ही रहेगा। वैज्ञानिकों ने ऐसी नौ बातें बताई हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनके नाम हैं - क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर का घटते जाना, समुद्रों में एसिडिटी बढ़ना, chemical pollution, fertilizer का इस्तेमाल, मीठे पानी की कमी, land conversion, biodiversity कम होना और air pollution. इनमें से चार तो खतरे के निशान को पहले ही पार कर चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है। हम इस नुकसान को कम भी कर सकते हैं और इसकी भरपाई भी। UN की तरफ से की गई स्टडीज ये बताती हैं कि साल 2100 तक दुनिया की आबादी लगभग 9.4 से 12.7 बिलियन के बीच होगी। लेकिन एनवायरमेंट अपनी लिमिट के हिसाब से ही लोगों को संभाल सकता है। इसलिए जब आबादी उस लिमिट से बढ़ जाती है तो इसे पुराने लेवल पर लाने के लिए कुछ लोगों का खात्मा जरूरी हो जाता है। ये बात हम जंगल और जानवरों के बारे में तो पक्के तौर पर समझते हैं पर परेशानी ये है कि इंसानों के साथ क्या होगा इसका हमें अंदाजा नहीं है। अगर समय रहते ही आबादी पर काबू नहीं पाया गया तो तबाही पक्की है।
अब यहां राहत इस बात की है कि हम आबादी को इतना बढ़ने से रोक सकते हैं। जब देश तरक्की की राह पर चलने लगते हैं तो पहले तो आबादी बढ़ती है फिर बढ़ना रुककर एक लेवल पर आ जाती है। जापान इसका एक अच्छा उदाहरण है। साल 2000 से अब तक इनकी आबादी बढ़ी ही नहीं है। अगर साल 1962 से डेटा लिया जाए तो दुनियाभर में आबादी बढ़ने की रफ्तार में कमी आती गई है। कभी न कभी हम भी उस जगह पर पहुंच जाएंगे। और ये जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। इसे जल्दी लाने का तरीका भी है। पहले तो महिलाओं की हालत सुधारने पर काम करना होगा। आज हालात बदल रहे हैं और महिलाएं इस बात का फैसला ले पा रही हैं कि उनको कितने बच्चे चाहिए और किस उम्र में। शिक्षा भी बड़ा रोल प्ले करती है। स्टडीज बताती हैं कि अगर हम शिक्षा पर ध्यान दें तो ये स्टेज लगभग 50 साल पहले ही आ सकती है। यानि आबादी में लगभग दो बिलियन लोगों की कमी। इससे हमारे एनवायरमेंट का बोझ काफी कम हो जाएगा।
अगर जंगल फलने फूलने लगें तो कार्बन घटेगी और बायो डायवर्सिटी बढ़ेगी। इससे भोजन की परेशानी का हल भी निकल आएगा।
जैसे जैसे बायो डायवर्सिटी कम होती गई वैसे वैसे हमारे प्लानेट की स्टेबिलिटी पर भी बुरा असर पड़ा। अब जबकि हमें ये अच्छी तरह पता है कि बायो डायवर्सिटी हमारे लिए कितनी जरूरी होती है तो इसे सही रखने के लिए जंगलों को फिर से बसाने की जरूरत है। समुद्रों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां किसी देश या इलाके की बाउंड्री नहीं है। इस बात की वजह से फिशिंग इंडस्ट्री ने मनचाहे तरीके से काम करते हुए मछलियों की ज्यादातर आबादी को खत्म कर दिया है। इसे रोकने के लिए ऐसे इलाकों को नो फिशिंग जोन बनाना चाहिए। इस तरह खुद ब खुद इतनी मछलियां पनप जाएंगी कि अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। लेकिन सिर्फ मछली पकड़ने पर रोक लगाना काफी नहीं है। किनारों का पानी न्यूट्रीशन से भरपूर होता है। इसलिए दुनियाभर में समुद्र के बीच जाकर ही नहीं बल्कि किनारों पर भी मछली पकड़ने की पाबंदी होनी चाहिए। ये तरकीब कैसे काम करती है इसका उदाहरण हमें मैक्सिको के Cabo Pulmo से मिल सकता है।
1990 तक इस इलाके में इतनी ज्यादा मछलियां पकड़ी जा चुकी थीं कि फिशिंग करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया था। तब इन लोगों ने मिलकर एक रास्ता निकाला। अपने इलाके में लगभग 7000 हेक्टेयर पर फिशिंग अगले 15 साल के लिए पूरी तरह से बंद कर दी। आने वाले कुछ साल तो मुश्किल से गुजरे। लेकिन फिर पानी में मछलियां बढ़ने लगीं। अगले 15 सालों में पहले से 400 गुना मछलियां हो गईं। खत्म हो चुकी शार्क भी वापस आ गई। 15 साल पूरे हो जाने पर मछुआरों को फिर से मछली पकड़ने की इजाजत दे दी गई लेकिन कुछ नियमों के साथ। अब वहां इतनी मछलियां पकड़ी जाने लगीं जितनी पहले कभी नहीं होती थीं। यहां डाइविंग और गेस्ट हाउस का काम भी चल निकला। हालांकि जमीन पर हालात बदलना मुश्किल होता है क्योंकि अक्सर इसका कोई न कोई मालिक होता ही है। हम जमीन की कीमत भी अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन ये बात कोई नहीं समझता कि जमीन, एनवायरमेंट के लिए कितनी कीमती हो सकती है। कागजों पर तो एक एकड़ पाम ऑयल के पेड़ों वाली जमीन एक एकड़ जंगल से कहीं ज्यादा कीमती है। पर हमें "वेल्यू" नाम के शब्द को सही तरह समझने की जरूरत है। जमीन पर कितनी फसल उग सकती है इसकी जगह हमें इसकी कीमत इस बात से लगानी चाहिए कि यहां कितनी बायो डायवर्सिटी है। अगर हम पहले ही ऐसा करते तो इतने जंगल कटते ही नहीं। लेकिन आज इतना करना ही काफी नहीं है। आगे हम कुछ और तरीकों पर बात करेंगे।
आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए ग्रीन और क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना सबसे कारगर कदम साबित हो सकता है।
धरती पर अभी तक हो चुके नुकसान को रोकने और इसकी भरपाई करने के लिए हमें पुराने तौर तरीकों पर वापस लौटना होगा। हमें नेचर से दूर होने की जगह नेचर के नजदीक जाना होगा। हमें ऐसी तकनीक पर काम करना होगा जो पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल की जगह ग्रीन एनर्जी पर चलती है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अल्बेनिया, पैराग्वे और आइसलैंड जैसे देश अब पूरी तरह ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। यानि अगर आप पक्का इरादा कर लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इंसानों ने इतनी तरक्की फॉसिल फ्यूल की बदौलत ही की है पर इसकी वजह से हवा में इतनी कार्बन छोड़ दी है जो वैसे लाखों सालों तक भी नहीं आती। हमने बिना सोचे समझे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके एक परेशानी और खड़ी कर दी है। आज हमारे पास दस साल से भी कम समय बचा है जब हम पेट्रोलियम को सूरज की रोशनी, पानी और हवा से बनी ग्रीन एनर्जी से बदल सकें। आज धरती का एवरेज तापमान 1℃ बढ़ चुका है। अगर हमें सब कुछ पहले की तरह करना है तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये 1.5℃ से ज्यादा न बढ़े। इस दशक के आखिर तक ये इस लेवल पर पहुंच ही जाएगा। हमने कुछ बदलाव तो किए हैं पर इनको सपोर्ट करने वाली तकनीक की कमी है।
एक बड़ी रुकावट तेल और गैस के सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं। आज लगभग हर बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट और कंपनियों के काम तेल और गैस के बिना अधूरे पड़ जाते हैं। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? बहुत से लोगों का मानना है कि कार्बन टैक्स लगा देना एक अच्छा कदम हो सकता है। यानि कोई कंपनी जितना ज्यादा कार्बन रिलीज करे वो उतना टैक्स देगी।
1990s में स्वीडन इस तरह की शुरुआत कर चुका है। इसके बाद से वहां ज्यादातर कंपनियों ने फॉसिल फ्यूल से दूरी बना ली। कार्बन कैप्चर टेक्नॉलॉजी भी फायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें हवा से कार्बन सोख ली जाती है। लेकिन इंसान के बनाए किसी तरीके से कहीं अच्छा है नेचुरल तरीका यानि पेड़ पौधे। अगर हम पेड़ पौधे लगाकर फिर से जंगलों को बसाना शुरू कर दें तो हवा से बहुत सी कार्बन ये पेड़ पौधे सोख लेंगे। अपना कल बेहतर बनाने के लिए हम सबको आज अपनी भागीदारी निभानी चाहिए।
कुल मिलाकर
पिछले कुछ दशकों में हमारी हरकतों की वजह से धरती और एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा है। हम तबाही के बहुत नजदीक आ चुके हैं। हमें जल्द से जल्द फॉसिल फ्यूल को ग्रीन एनर्जी से बदलने और बायो डायवर्सिटी को बढ़ाने की जरूरत है।
क्या करें
मीट और खास तौर पर बीफ के प्रोडक्शन में बहुत नेचुरल रिसोर्स लगते हैं। मीट और डेयरी से जुड़े कामों में दुनिया की खेती के लायक जमीन का लगभग 80% हिस्सा घिर जाता है। अगर हम मीट की खपत कम कर दें तो भी बहुत फर्क पड़ सकता है।
येबुक एप पर आप सुन रहे थे A Life on Our Planet By David Attenborough.
ये समरी आप को कैसी लगी हमें yebook.in@gmail.com पर ईमेल करके ज़रूर बताइये.
आप और कौनसी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं. हम आप की बताई गई समरी एड करने की पूरी कोशिश करेंगे.
अगर आप का कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें ईमेल करके ज़रूर बताएं.
और गूगल प्ले स्टोर पर ५ स्टार रेटिंग दे कर अपना प्यार बनाएं रखें.
Keep reading, keep learning, keep growing.