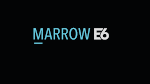William E. Paul, MD
जानिए हमारे इम्यून सिस्टम का महत्व
दो लफ्जों में
सुरक्षा इंसान की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। कुदरत ने हमें इम्यून सिस्टम के तौर पर एक ऐसा फंक्शन गिफ्ट किया है जो शरीर को सुरक्षित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साल 2015 में आई किताब इम्यूनिटी हमारे शरीर के इसी फंक्शन के बारे में बात करती है। ये किताब बताती है कि किस तरह इम्यून रिस्पांस हमें कई तरह की बीमारियों यहां तक कि कैंसर से भी बचाता है और इम्यून सिस्टम के कमजोर होने पर किस तरह के नुकसान हो सकते हैं।
ये किताब किनको पढ़नी चाहिए
- मेडिकल स्टूडेंट्स
- डॉक्टर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की फील्ड से जुड़े लोग
- हर वो इंसान जो कभी भी बीमार पड़ा हो
लेखक के बारे में
इस किताब के लेखक विलियम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज में इम्यूनोलॉजी लैब इंचार्ज के पद पर काम कर चुके हैं। ये इंस्टीट्यूट NIH में गिना जाता है। वे अमेरिकन असोसिएशन ऑफ इम्यूनोलॉजिस्ट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इम्यून सिस्टम के महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं।
हमारे आस-पास बीमारियों की ढेरों वजह मौजूद रहती हैं। खुली आंखों से न दिखने वाले वायरस, बैक्टीरिया जैसे जीव होते हैं। धूल, गंदगी और मिट्टी होती है। ये सब हमें तरह-तरह के इन्फेक्शन देने और बीमार करने के लिए काफी हैं। लेकिन इनके और हमारे बीच इम्यून सिस्टम एक ढाल बनकर अपना काम करता रहता है। इसको शरीर के दूसरे किसी फंक्शन से कम नहीं कहा जा सकता है। हम आगे इस सिस्टम को अच्छी तरह समझेंगे। इससे हमें ये समझने में भी आसानी होगी कि इम्यून सिस्टम की गड़बड़ जिंदगी के लिए एक बड़ा खतरा क्यों बन जाती है।
इम्यूनिटी बढ़ाने में टीकों के इस्तेमाल से लेकर कैंसर के खिलाफ लड़ाई में इम्यूनिटी की भूमिका तक ये किताब आपको इतिहास और विज्ञान की दुनिया की सैर कराती है। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे की कैसे अठारहवीं सदी में दूधवालों की वजह से टीकाकरण यानि वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई? म्यूकस का क्या महत्व है और
इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के क्या नुकसान हो सकते हैं!
तो चलिए शुरू करते हैं!
अगर कोई ये पूछे कि इम्यून सिस्टम अच्छा है या बुरा तो ज्यादातर लोग इसे अच्छा ही कहेंगे। आखिर ढेरों वायरस, बैक्टीरिया और बीमारियों से यही तो बचाता है। दवाइयां इसका काम और बेहतर बना देती हैं। लेकिन हर सिक्के की तरह इसके भी दो पहलू हैं। अगर ये सिस्टम ढंग से काम न करे तो इससे जान को खतरा भी हो सकता है। इसमें भी एक बैलेंस होना जरूरी है। यहां एक केस का जिक्र आता है जो इम्यूनोलॉजिस्ट के बीच बहुत फेमस है। स्मॉल पॉक्स यानि चेचक वायरस ने सदियों तक मानव जाति को परेशान कर रखा था। 8 मई 1980 को जब WHO ने इसके खात्मे का ऐलान किया उससे पहले तक ये लाखों लोगों की जान ले चुका था। लेकिन इसे कैसे हराया गया? वैक्सीनेशन की मदद से इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाकर।
वैक्सीनेशन वो तकनीक थी जिसे अठारहवीं सदी के डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने खोजा था। उन्होंने देखा कि दूधवालों को अक्सर काऊ पॉक्स का इन्फेक्शन होता था। ये बाकी लोगों को होने वाले चेचक से कम गंभीर होता था। जिन लोगों को एक बार काऊ पॉक्स हो गया उनको कभी चेचक नहीं होता था। एडवर्ड को पता था कि काऊ पॉक्स और चेचक वायरस में बहुत समानता है। उनको ख्याल आया कि अगर लोगों को काऊ पॉक्स से इन्फेक्ट करा दिया जाए तो उनको स्मॉल पॉक्स से बचाया जा सकता है। इस ख्याल ने वैक्सीनेशन को जन्म दिया। वैक्सीनेशन की मदद से हमारे शरीर का इम्यून रिस्पांस और मजबूत बनाया जाता है। इससे हमारा शरीर ऐसी सेल्स बनाता है जो बीमारियां और इन्फेक्शन फैलाने वाले जीवों से लड़ सकें। डॉक्टर जेनर की खोज के आधार पर WHO ने साल 1967 में चेचक के खात्मे के लिए अभियान शुरू किया। इसे ग्लोबल लेवल पर चलाया गया। इस अभियान में उम्मीद से कहीं बढ़कर सफलता मिली। लेकिन वैक्सीन जिस इम्यून रिस्पांस को बढ़ाती है वो उल्टा असर भी कर सकता है। डायबिटीज इसका एक उदाहरण है। आम तौर पर इम्यून सिस्टम उन सेल्स को टार्गेट करता है जो शरीर को नुकसान करें। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का शिकार हुए लोगों में इम्यून सिस्टम शरीर पर ही हमला करने लगता है। इस वजह से वो T cells जिनको वायरस को खत्म करना चाहिए वो शरीर में इन्सुलिन बनाने वाली सेल्स को ही खत्म करने लगती हैं। इसके नतीजे में डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी लग जाती है क्योंकि इन्सुलिन ब्लड शुगर लेवल सही रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इम्यूनिटी के नियम और इम्यून रिस्पांस तीन तरह के होते हैं।
आपने पढ़ा कि इम्यून सिस्टम जरूरी तो है लेकिन इसके कुछ खतरे भी हैं। पर इम्यून सिस्टम आखिर किसी इन्फेक्शन का सामना कैसे करता है? हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने वाले जीवों यानि पैथोजन के लिए तीन अलग-अलग तरह का इम्यून रिस्पांस होता है। पहला एक ऐसा बैरियर बनाना जो बैक्टीरिया जैसे किसी अटैक को सेल्स तक पहुंचने और उन्हें बीमार करने से पहले ही रोक दे। उदाहरण के लिए सांस की नली में एक चिपचिपी लाइनिंग होती है जिसे म्यूकस कहते हैं। आसान भाषा में आप इसे बलगम कह सकते हैं। सांस लेते समय हवा के साथ आए बैक्टीरिया इसमें फंस जाते हैं। इसके बाद वो या तो पेट में पंहुचकर एसिड में खत्म हो जाते हैं या खांसते और छींकते वक्त बाहर निकाल दिए जाते हैं।
दूसरी इम्यूनिटी हमें जन्म से मिलती है। इसे innate immunity कहा जाता है। इसे आप नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। इस तरह की इम्यूनिटी में कुछ खास सेल्स बैक्टीरिया जैसे खतरों का पता लगाने का काम करती हैं और दूसरी सेल्स को उनसे लड़ने के काम में लगा देती हैं।
तीसरी है अडॉप्टिव इम्यूनिटी। यानि ऐसी इम्यूनिटी जो हम समय के साथ डेवलप करते रहते हैं। इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ये भविष्य में होने वाले किसी खास अटैक के लिए आपको तैयार करती है। मान लीजिए आपको एक बार measles हुआ। अब ऐसी सेल्स बनेंगी जो इसका सामना करें। जब इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तब भी इनमें कुछ सेल्स शरीर में रह जाएंगी। ताकि दुबारा कभी measles के हमले के लिए शरीर पहले से तैयार रहे। इसलिए measles दुबारा नहीं होगा। क्योंकि आपका शरीर इसके खिलाफ पक्की दीवार बना चुका है। वैक्सीन भी इसी तरह की इम्यूनिटी देती है। अडॉप्टिव इम्यूनिटी हर इंसान में अलग हो सकती है और ये कुछ खास बीमारियों और पैथोजन पर ही असरदार होती है।
अब आपने ये तो समझ लिया कि इम्यून रिस्पांस किन तीन तरीकों से दिया जा सकता है। लेकिन इम्यून सिस्टम भी तीन नियमों पर चलता है। पहला नियम है कि इम्यून सिस्टम खास तरह की एंटीबॉडी बना सकता है। एंटीबॉडी वो सेल्स हैं जो बीमारी पैदा करने वाले कारणों को ढूंढती हैं और उन पर हमला करती हैं। यानि ये हर उस सेल को टार्गेट कर सकती हैं जिसे शरीर के लिए खतरा समझें। इस नियम को लॉ ऑफ universality कहा जाता है।
दूसरा नियम कहता है कि इम्यून सिस्टम अपने होस्ट पर अटैक नहीं करेगा। इसे लॉ ऑफ टॉलरेंस कहा जाता है। यानि इम्यूनिटी शरीर की हेल्दी सेल्स के खिलाफ काम नहीं करेगी। तीसरा नियम कहता है कि हर पैथोजन से अलग तरीके से निपटने की जरूरत है। इसे लॉ ऑफ appropriateness कहा जाता है। ये नियम इस बात का भी ध्यान रखता है कि इम्यून रिस्पांस कब देना है और किस तरह देना है। आगे हम इनके बारे में और डीटेल में पढ़ेंगे।
इम्यूनिटी का पहला नियम तो मेडिकल फील्ड में बीसवीं सदी की शुरुआत से ही चर्चा में रहा है।
इस पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इम्यून सिस्टम आखिर स्पेसिफिक तरीके से कैसे काम करता है? यानि ये अलग-अलग तरह के अटैक जिनको एंटीजन कहा जाता है के खिलाफ अलग-अलग तरह की एंटीबॉडी जैसा एडवांस डिफेंस कैसे बना लेता है?
इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें उन वैज्ञानिकों के बताए रास्ते पर चलना होगा जिन्होंने सबसे पहले इन नियमों को दुनिया के सामने रखा था। जर्मन वैज्ञानिक पॉल एर्लिच, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिसिटी देने वाले पहले इंसान थे। साल 1901 में एर्लिच ने ये कहा कि एंटीबॉडी उन्हीं मॉलीक्यूल्स तरह होती हैं जिन पर एंटीजन अटैक करते हैं। यानि एंटीजन अपना शिकार ढूंढते हुए गल्ती से एंटीबॉडी की तरफ भटक जाते हैं और एंटीबॉडी उनको खत्म कर देती हैं। ये थ्योरी देने के पीछे उनका ये कहना था कि एंटीबॉडी तो ब्लड में घूमती रहती हैं इसलिए एंटीबॉडी के लिए एंटीजन को उनके सही शिकार के पास पंहुचने से पहले ही खत्म करने का मौका होता है। हालाँकि उनकी थ्योरी में बहुत बड़ी गड़बड़ थी। असल में एर्लिच ने ये मान लिया था कि एंटीजन बस कुछ मुट्ठीभर होते हैं जो गिनी चुनी सेल्स को टार्गेट करते हैं। लेकिन कुछ ही सालों बाद ये बात सामने आई कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, प्रोटीन के साथ जुड़कर एंटीजन की तरह काम कर सकता है। यानि एंटीजन की आर्मी हमारी सोच से बहुत ज्यादा बड़ी है। एर्लिच की थ्योरी यहां दम तोड़ देती है।
1950 के दशक में डेविड टैल्मेज और फ्रैंक मैकफर्लेन बर्नेट नाम के वैज्ञानिकों ने स्पेसिफिसिटी की इससे बेहतर थ्योरी दी। इसका आधार थे लिम्फोसाइट्स यानि एक तरह के WBC जो अडॉप्टिव इम्यून रिस्पांस के लिए जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि हर लिम्फोसाइट में एक अलग एंटीजन रिसेप्टर होता है यानि वे अलग-अलग एंटीजन को पहचान सकते हैं। जबकि कुछ लिम्फोसाइट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी एंटीजन को पहचान सकते हैं।
इसलिए जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है और उसे कोई खास लिम्फोसाइट पहचान लेता है तो खास तरह की एंटीबॉडी बनने या "क्लोन" होने लगती हैं। इस थ्योरी को क्लोनल सलेक्शन कहा गया। इसे आज मेडिकल फील्ड में ज्यादातर लोग मानते हैं।
लॉ ऑफ टालरेंस ये समझाता है कि इम्यून रिस्पांस शरीर की हेल्दी सेल्स को ही टार्गेट बनने से कैसे रोकता है। ये बड़ी सामान्य सी बात है कि अगर घर पर कोई हथियार पड़ा होगा तो दुर्घटना के चांस होंगे ही भले ही आपने उसे सेल्फ डिफेंस के लिए क्यों न रखा हो। इससे बचने के लिए आप उसे लॉक करके रखेंगे, है ना? इसी तरह शरीर के पास एंटीबॉडी के रूप में भी तो हथियार ही होते हैं। इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है?
दरअसल शरीर में भी ऐसी दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं। इनको ऑटो इम्यून रिस्पांस कहा जाता है। पर इम्यूनिटी का दूसरा नियम, लॉ ऑफ टॉलरेंस इसे संभालता है। इसमें कुछ ऐसी सेल्स बनती हैं जो शरीर को खुद पर अटैक करने से रोक दें। इनको रेग्युलेटरी T सेल्स या "ट्रेग्स" कहा जाता है। ट्रेग्स, इन्फेक्शन से लड़ने वाली स्टैंडर्ड T सेल्स को कंट्रोल करते हैं। आप आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि ट्रेग्स ही स्टैंडर्ड T सेल्स को सही टार्गेट बताते हैं और उनको लिमिट में रखकर होस्ट को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं।
यानि जिन लोगों में ट्रेग्स न बनते हों या कोई खराबी हो उनमें ऑटो इम्यून रिस्पांस देखने को मिलता है। साल 2002 में आर एस वाइल्डिन, एस स्माइक-पियर्सन और ए एच फिलिपोविच नाम के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इसमें एक ऐसे बच्चे की केस स्टडी थी जिसे पैदा होने के कुछ ही दिनों में ऑटोइम्यून रिस्पांस ने अपना शिकार बना लिया। इसमें टाइप 1 डायबिटीज भी शामिल थी। उस बच्चे को पहले मिडिल इयर इन्फेक्शन हुआ। इसके बाद डायरिया और निमोनिया। जांच में ये पता चला कि इन सबके पीछे उसकी जीन्स में हुआ वो बदलाव था जिसने ट्रेग्स को बनने ही नहीं दिया।
चूहों पर किए गए प्रयोग में भी ऐसी घटनाएं भी देखी गई हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों, फियोना पॉवरी और डॉन मेसन ने चूहों की खास प्रजाति पर प्रयोग किए। इनको न्यूड रैट्स कहा जाता है। इनमें T सेल वाला इम्यून सिस्टम नहीं होता है। जब वैज्ञानिकों ने बिना ट्रैग्स वाली T सेल्स को सामान्य चूहों से न्यूड रैट्स में ट्रांसफर किया तो इन चूहों में ऑटोइम्यून रिस्पांस देखा गया। इससे ये पता चला कि T सेल्स की नुकसान पंहुचाने वाली ताकत को कंट्रोल करने के लिए ट्रेग्स का होना जरूरी है।
इम्यूनिटी का तीसरा नियम ये कहता है कि हर पैथोजन से निपटने के लिए एक सही इम्यून रिस्पांस की जरूरत होती है।
क्या आपने ये बात सुनी है कि पैथोजन हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में पाए जा सकते हैं और हमें कई तरह से बीमार कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। इनमें से कुछ तो सेल्स को इन्फेक्ट करके सीधे-सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो सेल्स के फंक्शन को ही बदल देते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों की वजह बनते हैं।
हर पैथोजन अलग होता है इसलिए उनके खिलाफ अलग तरह के इम्यून रिस्पांस की जरूरत होती है। ये बात हमें इम्यूनिटी के तीसरे नियम लॉ ऑफ appropriateness की तरफ ले जाती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सैन फ्रांसिस्को के एक वैज्ञानिक और डॉक्टर, रिचर्ड लॉकस्ली ने प्रयोगों से इसे साबित भी करके दिखाया है।
डॉक्टर लॉक्सली ने लीशमैनिया मेजर से इन्फेक्टेडेट चूहों पर प्रयोग किया। कुछ चूहों में इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया और कुछ में नहीं। लॉक्सली ने प्रयोग से ये साबित किया कि दोनों तरह के चूहों में इम्यूनिटी का ये लेवल इस बात पर आधारित था कि उनकी T सेल्स कितनी सही तरह काम करती हैं। ठीक हो जाने वाले चूहों में T सेल्स ने लीशमैनिया पैरासाइट पर ज्यादा अच्छी तरह काम किया था। अब सवाल ये उठता है कि इस फर्क की वजह क्या रही होगी?
इसकी वजह है डेन्ड्राइटिक सेल्स। ये सेल्स खतरा भांप लेती हैं और सही तरह का इम्यून रिस्पांस दिलवाती हैं। ये T सेल्स को एक्टिवेट करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं और ये लगभग हर टिशू में पाई जाती हैं। ये पहले इस बात को पहचानती हैं कि खतरा किस तरह का है। इसके बाद वो T सेल्स को मैसेज देती हैं कि उनको कैसा रिस्पांस देना है। मान लीजिए कि आपको फ्लू हो गया है। डेन्ड्राइटिक सेल्स इसके वायरस को पहचान लेंगी। अब ये ऐसी T सेल्स को ढूंढेंगी जो इस वायरस से सबसे अच्छी तरह लड़ सकें।
इम्यून सिस्टम, कैंसर से लड़ने में भी असरदार साबित हो सकता है।
कैंसर, मेडिकल फील्ड की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये एक तरह का ट्यूमर ही है जो जानलेवा साबित हो सकता है। इसमें सेल्स मनमाने ढंग से बढ़ने लगती हैं। इस पर वैज्ञानिक और डॉक्टर्स लगातार स्टडीज कर रहे हैं इस उम्मीद से कि एक दिन इसका नामोनिशान मिटाया जा सके। इनका मानना है कि इम्यून सिस्टम के पास इस समस्या का हल हो सकता है। बेहतर इम्यूनिटी, ट्यूमर की ग्रोथ को कम कर सकती है।
ताइवान में हुई एक स्टडी में ये पता चला कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से लिवर कैंसर की घटनाओं में काफी कमी आई है। इस वैक्सीनेशन की शुरुआत होने से पहले 1975 और 1976 के बीच पैदा हुए हर एक लाख लोगों में लिवर कैंसर की दर सालाना 0.64 परसेंट थी। लेकिन इसके बाद बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया जाने लगा था। इसलिए 1985 और 1986 के बीच पैदा हुए लोगों में ये परसेंट घटकर सिर्फ 0.1 रह गया। यानि इसमें भारी गिरावट देखने को मिली।
ये बदलाव कैसे आया? जाहिर सी बात है कि वैक्सीन की वजह से हुए इम्यून रिस्पांस ने कैंसर का खतरा कम करने में मदद की होगी। मेडिकल फील्ड में ऐसे ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। सिएटल के एक अस्पताल में रिचर्ड प्रेन और जोन मेन ने 1950 के दशक में एक प्रयोग किया। इस स्टडी में ये पाया गया कि ट्यूमर में खास एंटीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से शरीर इम्यून रिस्पांस देता है और सही एंटीबॉडी बन जाएं तो कैंसर का सामना किया जा सकता है।
इस प्रयोग में चूहों को कैंसर पैदा करने वाले केमिकल से एक्सपोज किया गया। जब चूहों के ट्यूमर तय आकार तक बढ़ जाते तो वैज्ञानिक उन्हें सर्जरी करके निकाल देते। कुछ दिनों बाद ट्यूमर को कैंसर वाले और हेल्दी दोनों चूहों में वापस डाला जाता।
बारह में से दस हेल्दी चूहों में ट्यूमर फैलने लगा। लेकिन जिन चूहों को पहले से कैंसर था उनमें ये ट्यूमर खत्म हो गया। यानि इन चूहों में अब इस तरह के कैंसर के खिलाफ इम्यूनिटी बन चुकी थी। इस तरह के नतीजे ये उम्मीद जगाते हैं कि कैंसर से लड़ाई जीती जा सकती है।
कुल मिलाकर
इम्यून सिस्टम किसी वरदान से कम नहीं। पर इसकी गड़बड़ भी उतनी ही नुकसानदायक हो सकती है। इम्यून सिस्टम को अच्छी तरह समझकर वैज्ञानिकों ने ढेरों बीमारियों का इलाज ढूंढकर उन पर काबू पा लिया है। हो सकता है कि आगे चलकर ये कैंसर को जड़ से मिटाने में भी मदद करे।
येबुक एप पर आप सुन रहे थे Immunity By William E. Paul, MD.
ये समरी आप को कैसी लगी हमें yebook.in@gmail.com पर ईमेल करके ज़रूर बताइये.
आप और कौनसी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं. हम आप की बताई गई समरी एड करने की पूरी कोशिश करेंगे.
अगर आप का कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें ईमेल करके ज़रूर बताएं.
और गूगल प्ले स्टोर पर ५ स्टार रेटिंग दे कर अपना प्यार बनाएं रखें.
Keep reading, keep learning, keep growing.